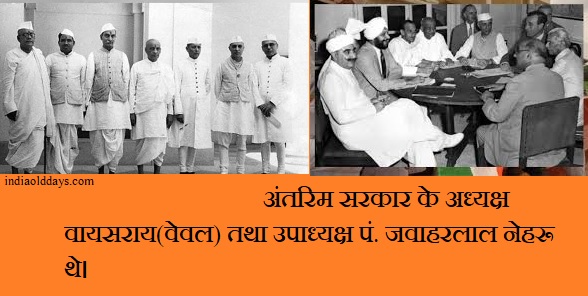मुगल वंश का संस्थापकः बाबर( 1526-1530 )

बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ई. को मावराउन्नहर ( ट्रान्स अक्सियाना ) की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमरशेख मिर्जा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था। तथा उसकी माँ का नाम कुतलुगनिगार खाँ था। बाबर पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का पाँचवां वंशज तथा मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खाँ का चौदहवा वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था।
बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली, वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। जिसका नाम चंगेज खाँ के द्वितीय पुत्र के नाम पर पङा था।बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494ई. में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उजबेगों से बार-2 पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर की उजबे सरदार शैबानी खाँन ने बार-2 पराजय उसे अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोङकर दक्षिण पूर्व भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए विवश कर दिया। इसी कङी में बाबर ने 1504ई. में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणामस्वरूप उसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि करता था।
बाबर के भारत पर आक्रमण निम्नलिखित हैं –
बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाङ, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विच्छन्न बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल पाँच मुस्लिम शासकों-
- बंगाल,
- दिल्ली,
- मालवा,
- गुजरात एवं
- बहमनी राज्यों
तथा दो हिन्दू शासकों – मेवाङ एवं विजयनगर का ही उल्लेख किया है।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ लोदी तथा इब्राहीम के चाचा आलम खाँ लोदी ने दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पायी है। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर चार बार आक्रमण किया था। और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इस किले ( भेरा ) को जीतने में उसने सर्वप्रथम युद्ध ( 21 अप्रैल 1526 ) में बाबर की विजय के मुख्य कारण – उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उजबेगों की युद्ध नीति तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि ( रूमी विधि ) का प्रयोग किया था। दो गाङियों के बीच व्यवस्थित जगह छोङकर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि को उस्मानी विधि इसलिए कहा जाता था, क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति उजबेकों से ग्रहण की थी।
पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खाँ नामक दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहीम लोदी की पराजय के मुख्य कारण – एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफागान सरदारों की उससे क्षुब्धता थी।
पानीपत का युद्ध – इस युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक-2 चाँदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता था।
राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लङे गये खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था।
राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा से 40 किमी. दूर खानवाँ नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ई. को हआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खाँ मेवाती, महमूद लोदी, आलमा खाँ लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बुझाने केलिए जिहाद ( इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म -युद्ध ) का नारा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी ( योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों ) की उपाधि धारण की थी।
आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा की सेनाओं में 1ः2 का अनुपात बताया है। बाबर ने 29 जनवरी 1528ई. में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनीराय पर आक्रमण कर दिया। मेदिनीराय पराजित हुआ, यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई।बाबर ने इस युद्ध के अवसर पर भी – जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध के पश्चात् राजपूतों के सिरों की मीनार बनवायी थी। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था। बाबर ने 6 मई 1529 ई. में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया।
इस युद्ध के पश्चात् बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिन्धु से लेकर बिहार तक तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गया। 26 दिसंबर 1530 ई. में आगरे में बाबर की मृत्यु हो गयी और उसे आगरा में नूर-अफगान ( आधुनिक आरामबाग ) बाग में दफना दिया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गये स्थान पर दफनाया गया।
बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि – काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं। जिसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है।
बाबर के भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कंधार सम्मिलित हुए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी (तुर्की ) में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहीम लोदी की माँ द्वारा दिये गये विष को मानते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोङकर अपने को बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पूर्व के शासक अपने को सुल्तान कहकर ही पुकारते थे।
बाबर द्वारा किये गये लोकहित के कार्य-
बाबर बागों को लगाने का बङा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूरे-अफगान कहा जाता था। परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने सङकों को नापने के लिए गज-ए-बाबरी नामक माप का प्रयोग किया, जो कालांतर तक चलता रहा।
बाबर की आत्मकथा-
बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इर्सिकन सहित अब्दुर्रहीम खानखाना ने फारसी और श्रीमती बेबरिज ने अंग्रेजी में किया। एलफिंस्टन ने उसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि – “वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। “बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान (तुर्की भाषा) का संकलन करवाया।
बाबर ने मुबइयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। उसने रिसाल-ए-उसज की रचना की जिसे खत-ए-बाबरी भी कहा जाता है। बाबर के बारे में लेनपूल ने लिखा कि “Babur was a mere soldier of farture and not the founder of an empire” ।
Reference : https://www.indiaolddays.com/