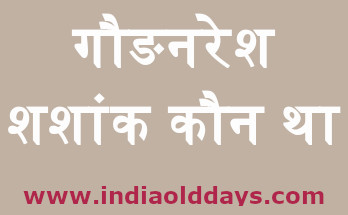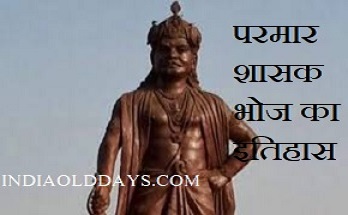टाउनशेड शुल्कों के हटा लिये जाने के बाद उपनिवेशियों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। अभी भी अमेरिका में इंग्लैण्ड के प्रति काफी सद्भावना थी, विशेषकर धनिक वर्गों में। स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराए गये दंगों तथा बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि गङबङ से व्यापार को हानि पहुँचती थी।
साधारण अमेरिकी को भी इंग्लैण्ड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अधिक इच्छा न थी, वह तो केवल यह चाहता था, कि अपने खेत या दुकान पर आजादी से काम करे और शांति से अपना निर्वाह करे, परंतु देशभक्तों तथा अतिवादियों का एक छोटा-सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था।
उनका कहना था, कि जब तक चाय-कर रहेगा, उपनिवेशियों पर इंग्लैण्ड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा और इसकी आङ में भविष्य में कभी भी इस सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशियों की स्वतंत्रता के लिये घातक सिद्धांत का डटकर विरोध किया जाना चाहिये। संयोग से उग्रवादियों को सैमुअल एडम्स जैसा आदर्श नेता मिल गया। उसमें साहस और कुशल बुद्धि भी थी।
उसकी वाक्य-शैली सुस्पष्ट और निष्कपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थन भी प्राप्त था। उसका मुख्य ध्येय अमेरिकी लोगों को अपने महत्त्व का आभास कराना और उन्हें आंदोलन के लिए जागृत करना था। इसके लिये उसने लेखों तथा भाषणों का सहारा लिया और पत्र-व्यवहार समितियों की स्थापना की। ऐसे ही समय में इंग्लैण्ड की सरकार की एक भारी भूल ने असंतोष की ज्वाला को पुनः प्रज्जवलित कर दिया।
इंग्लैण्ड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा इस समय संकटापन्न हो गयी थी। कंपनी को इंग्लैण्ड की आवश्यकतानुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु इस समय इंग्लैण्ड के गोदामों में चाय भरी थी। उसका कोई ग्राहक ही न था। दि कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार मिल जाये तो कंपनी दिवालिया होने से बच सकती थी।
वैसे भी अमेरिका में 1770 ई. के बाद से ही चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ गया था, अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 ई. में संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया।
उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था। आशा यह थी, कि उपनिवेशी सस्ती चाय बङी मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानी पहुँच रही थी, अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुँचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई न था। विवश होकर अधिकांश जहाजों को वापस इंग्लैण्ड भेजना पङा, परंतु बॉस्टन बंदरगाह में कुछ जहाज रुक गए।
बॉस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर, 1773 ई. की रात को पचास-साठ व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष धारण करके जहाजों पर धावा कर दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना इतिहास में बॉस्टन टी-पार्टी के नाम से विख्यात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के एक कानून का पालन करते हुये काम किया था।
उपनिवेशियों ने संसद की अवहेलना करके उसके अधिकार को चुनौती दी। जार्ज तृतीय जैसा शासक इस प्रकार की कार्यवाही को कभी सहन नहीं कर सकता था और न ही संसद इसे सहन कर सकती थी, अतः संसद ने पाँच निष्ठुर नियम पास किए जिनका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। पहले नियम के द्वारा बॉस्टन बंदरगाह को उस समय तक के लिये बंद कर दिया गया, जब तक चाय का हर्जाना न दे दिया जाये।
इससे बॉस्टन नगर का जन-जीवन ही संकटमय हो गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था, बॉस्टन का आर्थिक विनाश। दूसरे नियम के अंतर्गत मेसाचूसेट्स के सभासदों, जिन्हें पहले उपनिवेशी निर्वाचित करते थे, को नियुक्त करने का अधिकार राजा को दिया गया। गवर्नर को न्यायाधीश नामांकित करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर की अनुमति के बिना नगरसभाओं की बैठक पर रोक लगा दी गयी।
तीसरे नियम के अंदर हत्या संबंधी मुकदमे इंग्लैण्ड या अन्य उपनिवेशों में न्याय हेतु भिजवाने का प्रावधान था। चौथे नियम के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिये समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों के ऊपर डाल दिया गया। पाँचवें नियम के द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान की गयी और क्वीबेक की सीमा आहियो नदी तक बढा दी गयी।

1. पुस्तक- आधुनिक विश्व का इतिहास (1500-1945ई.), लेखक - कालूराम शर्मा