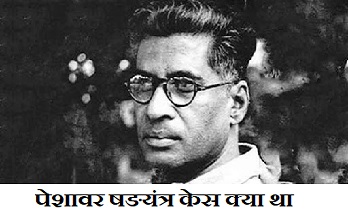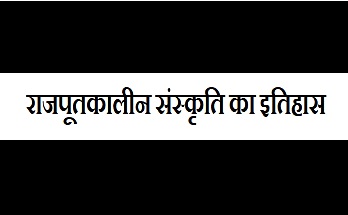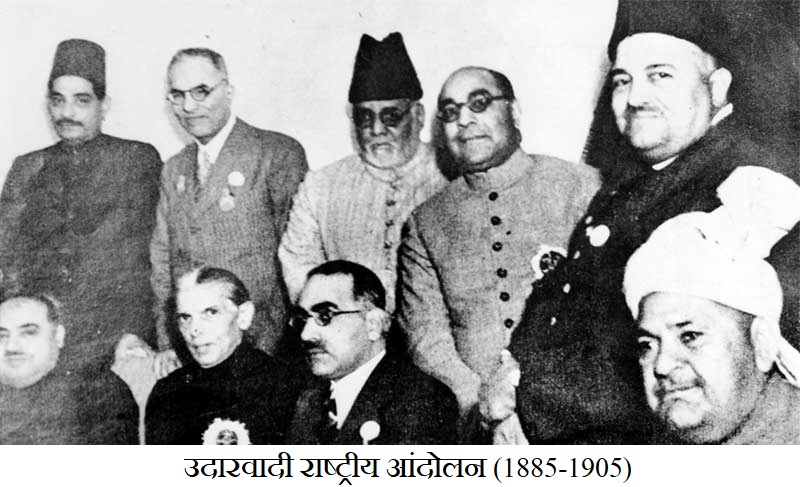मुसोलिनी की विदेश नीति
पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की उपेक्षा की गयी। इटली फ्यूम पर अधिकार करना चाहता था, किन्तु वह उसे प्राप्त नहीं हुआ।1920 में उसे अल्बानिया से अपनी सेना हटानी पङा।
स्पा सम्मेलन में इटली के लिये क्षतिपूर्ति की रकम केवल 10 प्रतिशत निश्चित की गयी।अगस्त, 1920 में सेर्बे की संधि हुई, किन्तु इससे भी इटली को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 12 नवंबर, 1920 को रेपोलों की संधि हुई जिसके द्वारा फ्यूम को स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया गया। रेपोलो की संधि इटली का राष्ट्रीय अपमान था।
इससे इटली में चारों ओर असंतोष की लहर के कारण ही शक्ति संपन्न हुआ था। अतः मुसोलिनी ने उग्र विदेश नीति का अनुसरण किया, जिसका लक्ष्य इटली को अन्तर्राष्ट्रीय जनगत में गौरवपूर्ण स्थान दिलाना, भूमध्यसागर को इटली की झील बनाना, अफ्रीका में विशाल साम्राज्य स्थापित करना तथा वर्साय संधि में संशोधन करना था।

भूमध्य सागर पर प्रभुत्व का प्रयास
पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली ने भूमध्यसागर के पूर्वी भाग में स्थित रोहड्स तथा डाडेक्नीज द्वीप समूहों को प्राप्त करने का प्रयास किया था, किन्तु वहाँ इटली की माँग को अस्वीकृत कर दिया गया था और सेर्बे की संधि द्वारा इन द्वीप समूहों पर से इटली को अपने दावे का परित्याग करना पङा था।
मुसोलिनी भूमध्यसागर में पूरी प्रभुसत्ता स्थापित कर उसे रोमन झील के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। परिणामस्वरूप 24 जुलाई, 1923 को ल्युसेन (लोसाने) की संधि हुई, जिसके द्वारा सेर्बे की संधि में संशोधन किया गया तथा इटली को रोहड्स और डाडेक्नीज द्वीप समूह प्रदान किए गए।
वह मुसोलिनी की विदेश नीति की प्रथम सफलता थी। इन द्वीप समूहों में उसने सुदृढ किलेबंदी की और एक अच्छा नौ सैनिक अड्डा तैयार कर लिया।
कोर्फ्यू काण्ड

अल्बानिया और यूनान की सीमा निर्धारण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया था। 23 अगस्त, 1923 को यूनान की सीमा पर झगङा हो गया और गोली चल गई, जिससे एक इटालियन सैनिक अधिकारी तथा चार अन्य इटालियन मारे गए।
मुसोलिनी ने यूनान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वह इटालियन अधिकारियों की सहायता से मामले की जाँच करे, पाँच दिन के अन्दर दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया जाय, यूनानी झंडा इटली के झंडे के समक्ष झुकाया जाय और पाँच करोङ लीरा इटली को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाय।
यूनान ने इन माँगों को अस्वीकार कर दिया तथा मामले को राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किया। किन्तु मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुये 31 अगस्त, 1923 को यूनान के कोर्फ्यू टापू पर बमवर्षा करके उस पर अधिकार कर लिया। जब इटली ने इस मामले में राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का विरोध किया तो मामला राजदूतों के सम्मेलन को सौंप दिया गया।
इस सम्मेलन ने यूनान को क्षमा याचना एवं पाँच करोङ लीरा क्षतिपूर्ति देने को भी कहा और इटली को कोर्फ्यू से अपनी सेनाएँ हटाने को कहा। मुसोलिनी ने इन निर्णयों को स्वीकार करने में आनाकानी की, किन्तु ब्रिटेन द्वारा इटली को चेतावनी देने पर उसने इन निर्णयों को स्वीकार करने में आनाकानी की, किन्तु ब्रिटेन द्वारा इटली की चेतावनी देने पर उसने इन निर्णयों को स्वीकार कर लिया और 27 सितंबर को टापू खाली कर दिया।
राष्ट्रसंघ की उपेक्षा ने तथा विशाल क्षतिपूर्ति की प्राप्ति ने मुसोलिनी को इटली में लोकप्रिय बना दिया।
फ्यूम की प्राप्ति
पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्यूम बंदरगाह तथा यूनान के प्रश्न पर इटली व यूगोस्लाविया के बीच घोर मतभेद उत्पन्न हो गया था। मित्र राष्ट्रों के प्रयत्नों से 1920 में रेपोलों की संधि हुई, जिसके द्वारा फ्यूम को एक स्वतंत्र बंदरगाह घोषित कर दिया गया।
मुसोलिनी ने 27 जनवरी, 1924 को यूगोस्लाविया के साथ रोम की संधि की। इस संधि के अनुसार फ्यूम का नगर तो इटली को प्राप्त हो गया तथा एक छोटी नदी द्वारा पृथक होने वाला फ्यूम का उपनगर बारोस बंदरगाह तथा सूशाक की बस्ती यूगोस्लाविया को प्राप्त हुई। इस प्रकार मुसोलिनी ने फ्यूम का प्रश्न हल करके बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त की।
अल्बानिया पर प्रभुत्व
मुसोलिनी एड्रियाटिक सागर पर पूरा अधिकार स्थापित करना चाहता था, किन्तु इसके लिये ओट्रेण्डो के जलडमरुओं पर नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक था। अतः 27 नवम्बर, 1926 को अल्बानिया की राजधानी टिराना में एक संधि हुई, जिसके द्वारा अल्बानिया ने यह स्वीकार कर लिया कि वह दूसरे देशों के साथ इटली को हाने पहुँचाने वाला कोई राजनैतिक या सैनिक समझौता नहीं करेगा।
1927 में इटलियन सैनिक अधिकारियों द्वारा अल्बानिया की सेना का पुनर्गठन किया गया तथा इटली ने अल्बानिया के साथ 20 वर्ष का एक रक्षात्मक समझौता कर लिया जिससे अल्बानिया इटली का संरक्षित राज्य बन गया। मुसोलिनी धीरे-धीरे अल्बानिया में अपना प्रभुत्व बढाचा रहा और अंत में 1939 में उसने इस पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया।
टैंजियर संकट
मोरक्को के टैंजियर में बंदरगाह में अन्तर्राष्ट्रीय शासन था। अक्टूबर, 1927 में शासन में संशोधन करने के प्रश्न पर विार करने के लिये यहाँ फ्रांस व स्पेन के प्रतिनिधि एकत्र हुए।इसी समय तीन इटालियन युद्धपोत भी वहाँ पुहँच गए और रोम से घोषणा की गयी कि भूमध्यसागर की एक शक्ति के रूप में टैंजियर के विषय में इटली को भी गहरी दिलचस्पी है।
रोम में हुई घोषणा के फलस्वरूप इटली को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और 1928 में टैंजियर के संबंध में हुए नए समझौते में इटली को इस नगर के प्रशासन में अधिक अधिकार प्रदान किए गये। इस प्रकार अब इटली महाशक्तियों की पंक्ति में आ गया। यह मुसोलिनी की भारी कूटनीतिक विजय थी।
1930 में लंदन के नौसैनिक सम्मेलन में इटली ने भूमध्यसागर में फ्रांस के समान नौ सेना रखने के अधिकार की माँग की।
रूस से मित्रता
मुसोलिनी ने अब भूमध्यसागर में अपनी स्थिति सुदृढ करने का प्रयास आरंभ कर दिया। वह अपना पक्ष सबल बनाने के लिये यूरोप में शक्तिशाली मित्र प्राप्त करना चाहता था। यूरोप के अधिकांश देश यथास्थिति के समर्थक एवं शांति समझौते के संशोधन के विरोधी थे। यद्यपि जर्मनी भी संधि में संशोधन चाहता था, किन्तु उसकी दशा अत्यन्त ही कमजोर थी।
आस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया, इटली से घनिष्ठता स्थापित करने लगे।किन्तु ये सभी छोटे राज्य थे। बङे राष्ट्रों में केवल रूस बचा था जो संधि में संशोधन का पक्षपाती था। अतः मुसोलिनी ने फरवरी, 1924 में रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करके उसके साथ व्यापारिक संधि कर ली थी।
इटली अब रूस को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद मुसोलिनी ने अप्रैल, 1927 में हंगरी के साथ 23 दिसंबर, 1928 को यूनान के साथ और 6 फरवरी, 1930 को आस्ट्रिया के साथ मित्रता की संधियाँ की।
हिटलर का उत्कर्ष एवं फ्रांस-ब्रिटेन से सहयोग
1933 के आरंभ में जर्मनी में हिटलर सत्तारूढ हुआ जिससे समस्त विश्व में एक राजनैतिक क्रांति हुई। मुसोलिनी भी हिटलर के उत्थान से भयभीत हुआ, क्योंकि हिटलर आस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिलाना चाहता था, किन्तु मुसोलिनी चाहता था कि आस्ट्रिया पर इटली का प्रभाव बना रहे।
यदि आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो जाता तो दक्षिणी टाइरोल को जो वर्साय संधि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था खतरा पैदा हो सकता था। अतः जर्मनी में हुई नाजी क्रांति के फलस्वरूप इटली की विदेश नीति में भी परिवर्तन आया। इक तरफ तो उसने इंग्लैण्ड और फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति को अपनाया और दूसरी तरफ उसने आस्ट्रिया के साथ समझौता कर उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया।
मुसोलिनी अपनी तरफ से आस्ट्रिया के नाजी विरोधियों को हर प्रकार की सहायता देने लगा। जुलाई, 1934 में हिटलर ने आस्ट्रिया में राजनैतिक विद्रोह कराकर आस्ट्रिया के विलय की योजना बनाई, किन्तु मुसोलिनी ने आस्ट्रिया की सीमा पर अपनी सेना तैनात करके घोषणा की कि यदि जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया तो इसका अर्थ होगा इटली के साथ युद्ध।
इससे हिटलर भयभीत हो गया और उसने घोषणा की कि इस घटना में जर्मनी का कोई हाथ नहीं था। इस प्रकार मुसोलिनी ने हिटलर की आस्ट्रिया विलय की योजना पर पानी फेर दिया। युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण फ्रांस और इटली के संबंध में निरंतर बिगङते जा रहे थे, किन्तु आस्ट्रिया पर हिटलर की गिद्ध दृष्टि एक ऐसा खतरा था, जिससे दोनों ही देश अब समझौता करना ही सही समझते थे। अतः 7 जनवरी, 1935 को फ्रांस और इटली के बीच समझौता हो गया। इस समझौता के अनुसार
फ्रांस ने अफ्रीका से सुमालीलैण्ड तथा लीबिया के पास का कुछ क्षेत्र इटली को दे दिया।
समझौते में यह निर्णय लिया गया कि यदि जर्मनी अपना शस्त्रीकरण करेगा तो दोनों देश मिलकर इस संबंध में विचार करेंगे।
इस अवसर पर फ्रांस का विदेश मंत्री लावल रोम आया था और मुसोलिनी ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। ऐसा विश्वास किया जाता है, कि लावल ने मुसोलिनी को यह आश्वासन दिया था कि अबीसीनिया में फ्रांस का कोई हित नहीं है।
इस प्रकार फ्रांस ने परोक्ष रूप से इटली को अबीसीनिया पर अधिकार करने की छूट दे दी। मार्च, 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुये जर्मनी के शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। अतः स्विट्जरलैण्ड के स्ट्रेसा सम्मेलन की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया। स्ट्रेसा में उन्होंने हिटलर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा कायम किया।
वस्तुतः सम्मेलन के प्रतिनिधियों में एकता नहीं थी। एक ओर हिटलर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया जा रहा था और दूसरी ओर सुंक्त मोर्चे का एक सदस्य इंग्लैण्ड जर्मनी के साथ ही नौ सेना संबंधी समझौता करने के लिये वार्ता कर रहा था।
अबीसीनिया पर आक्रमण
1930-32 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण इटली की आर्थिक स्थिति भी बिगङती जा रही थी तथा 1934 तक लगभग ढाई लाख लोग बेकार हो गये थे। अतः जनता का इस आर्थिक समस्या से ध्यान दूसरी ओर बँटाना आवश्यक था। इसके लिये उसने अफ्रीका के एकमात्र स्वतंत्र, किन्तु निर्बल देश, अबीसीनिया को चुना।
1896 में इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य से मिलाने का प्रयत्न किया, था, किन्तु अडोवा के युद्ध में इटली को बुरी तरह पराजित होना पङा था। मुसोलिनी अडोवा की पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता था।
इरिट्रिया, लीबिया और सोमालीलैण्ड में इटली का प्रभुत्व पहले ही स्थापित हो चुका था और अब यदि अबीसीनिया भी उसमें सम्मिलित हो जाता है तो अफ्रीका में इटली का विशाल साम्राज्य स्थापित हो सकता था। अबीसीनिया में तरह-तरह के खनिज पदार्थ उपलब्ध थे जिससे इटली का औद्योगिक विकास हो सकता था।
इसके अलावा इटली की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। अतः बढती हुई आबादी को बसाने के लिये उसे अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता थी और इसके लिये अबीसीनिया एक अच्छा प्रदेश था। अतः मुसोलिनी उस पर आक्रमण करने की सोचने लगा।
मुसोलिनी की इस इच्छा में सबसे बङा बाधक फ्रांस था, किन्तु हिटलर के उत्कर्ष के कारण अब दोनों में मित्रता हो चुकी थी। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और इस अवसर पर राष्ट्रसंघ का खोखलापन प्रकट हो चुका था, जिससे मुसोलिनी का हौंसला बढ गया।
उधर हिटलर ने वर्साय संधि को अमान्य घोषित करते हुये उसकी धाराओं को तोङना आरंभ कर दिया था, किन्तु उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इन परिस्थितियों से मुसोलिनी को प्रेरणा मिली और उसने अबीसीनिया पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया।
5 दिसंबर, 1934 को इटालियन सोमालीलैण्ड और अबीसीनिया की अनिश्चित सीमा पर वालवाल नामक स्थान पर हुए एक सैनिक झगङे में तीस इटालियन मारे गए। मुसोलिनी के लिये यह स्वर्ण अवसर था। उसने अबीसीनिया में क्षमा याचना करने और क्षतिपूर्ति की माँग की।
किन्तु अबीसीनिया ने यह मामला मध्यस्थ को सौंपने पर बल दिया और 14 दिसंबर को उसने राष्ट्रसंघ में इटली के आक्रमण की शिकायत की। राष्ट्रसंघ ने कुछ समय तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि राष्ट्रसंघ का एक प्रभावशाली सदस्य फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध, इटली को अपना मित्र बनाने को उत्सुक था।
3 जनवरी, 1935 को कौंसिल की बैठक में अबीसीनिया ने यह प्रश्न पुनः उठाया और इटली इस मामले को पंच निर्णय के लिये सौंपने को तैयार हो गया। 3 सितंबर, 1935 को इन पंचों के कमीशन ने निर्णय दिया कि वालवाल की घटना के लिये इटली और अबीसीनिया दोनों उत्तरदायी नहीं हैं।
अब कौंसिल की बैठक में पंचों के कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा था तब इटली के प्रतिनिधि ने अबीसीनिया पर विश्वासघात और संधि भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि हम इन असभ्यों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। यह कहते हुये इटली के प्रतिनिधि ने कौंसिल की बैठक का परित्याग कर दिया।
4 दिसंबर, 1935 को कौंसिल ने उक्त रिपोर्ट के साथ इस प्रश्न पर विचार समाप्त कर दिया। किन्तु मुसोलिनी अबीसीनिया पर अधिकार करनेपर तुला हुआ था, चाहे यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो, उसकी बिना सहायता के हो अथवा उसका विरोध करके हो।
मुसोलिनी ने अबीसीनिया की सीमा पर सेनाएँ एकत्र करना आरंभ कर दिया। इस पर अबीसीनिया ने पुनः राष्ट्रसंघ में शिकायत की। इस पर कौंसिल ने इस विवाद को हल करने के लिये पाँच देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैण्ड, स्पेन और टर्की) की एक समिति नियुक्त की।
इसने इटली को संतुष्ट करने के लिये अबीसीनिया में इटली के विशेष आर्थिक अधिकार को मानते हुए अबीसीनिया के कुछ प्रदेश इटली को देने का प्रस्ताव किया। किन्तु मुसोलिनी ने कहा, यदि संपूर्ण अबीसीनिया भी मुझे चाँदी की थाली में भेंट किया जाय तो मैं उसे अस्वीकार कर दूँगा, क्योंकि मैंने इसे शक्ति से लेने का निर्णय कर लिया है।
इसी बीच मुसोलिनी ने अबीसीनिया की सीमा पर भारी मात्रा में सेनाएँ एकत्र कर ली। अतः 29 सितंबर को अबीसीनिया के सम्राट हेलीसिलेसी ने आत्म रक्षा के लिये लामबंदी की आज्ञा दे दी। इस पर मुसोलिनी ने कहा कि अबीसीनिया ने इटली पर हमला कर दिया है अतः हम भी अपनी आत्मरक्षा के लिये युद्ध करेंगे और 1 अक्टूबर, 1935 को अपनी सेनाओं को अबीसीनिया पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी।
6 अक्टूबर, 1935 को इटली की सेनाओं ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। 7 अक्टूबर, 1935 को इटली की सेनाओं ने अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। 7 अक्टूबर को कौंसिल की एक समिति ने इटली पर युद्ध आरंभ करने का उत्तरदायित्व डाला। 9 अक्टूबर, से 11 अक्टूबर, तक राष्ट्रसंघ के लगभग 50 सदस्य इस समस्या पर विचार करते रहे।
अंत में कौंसिल के प्रस्ताव पर इटली को आक्रामक घोषित किया गया तथा इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिये 18 व्यक्तियों की एक समिति गठित कर दी। इस समिति ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जिन्हें इटली में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया।
इस सूची में जानबूझ कर तेल को सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे इटली को बराबर तेल प्राप्त होता रहा। इन प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने की बात कही गयी थी किन्तु ये प्रतिबंध 18 नवम्बर से लगाए गए। वस्तुतः फ्रांस की सहानुभूति इटली के साथ थी अतः इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध पूर्ण शक्ति के साथ नहीं लगाए गए।
ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही मुसोलिनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना रहे थे। सितंबर, 1935 में फ्रांस के विदेश मंत्री लावल तथा ब्रिटेन के विदेश मंत्री सेमुअल होर ने यह गुप्त समझौता किया कि यदि राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा तो वे सिद्धांत रूप से इसका समर्थन करते हुये भी इटली के लिये स्वेज नहर बंद करने का तथा सैनिक कार्यवाही का विरोध करेंगे।
नवम्बर-दिसंबर, 1935 में जब संघ तेल भेजने पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहा था तब इन दोनों राजनीतिज्ञों ने पेरिस में 7 दिसंबर, 1935 को एक गुप्त समझौता किया, जिसमें कहा गया कि अबीसीनिया के प्रश्न पर इटली से युद्ध मोल लेना उचित नहीं है, अतः इटली को तेल भेजने के प्रतिबंध को लागू करने की कार्यवाही में विलम्ब करना चाहिये।
इस समझौते में यह भी कहा गया कि अबीसीनिया को कहा जाय कि वह इटली को इरिट्रिया व सोमालीलैण्ड के पास कुछ प्रदेश दे दे, दक्षिणी अबीसीनिया को इटली के आर्थिक विस्तार एवं बस्ती के लिये सुरक्षित रखा जाय और इसके बदले में इटली, अबीसीनिया को समुद्र तट तक निकास के लिये लाल सागर पर एक बंदरगाह दे दे।
होर-लावल समझौता राष्ट्रसंघ के महान आदर्शों के प्रति विश्वासघात था। यह समझौता अत्यन्त ही गुप्त रखा गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश यह गुप्त समझौता समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया। ब्रिटेन में इस पर इतना रोष हुआ कि विदेश मंत्री होर को त्याग पत्र देना पङा।
जनवरी, 1936 में इटली की सेनाएँ अबीसीनिया में निरंतर आगे बढती गई। इटली ने केवल आक्रमण ही नहीं किया बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध संबंधी नियमों का खुले आम उल्लंघन किया। विमान से ऐसी गैसें गिराई गई तथा ऐसी गोलियों का प्रयोग किया गया जिनका प्रयोग युद्ध नियमों के अनुसार निषिद्ध था।
परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक स्थान पर अबीसीनिया की सेना पराजित होने लगी। 1 मई, 1936 को इटली की सेनाओं ने अबीसीनिया की राजधानी आदिम अबाबा पर अधिकार कर लिया। सम्राट हेलीसिलेसी राजधानी छोङकर भाग खङा हुआ। 9 मई, 1936 को अबीसीनिया को इटली के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया।
30 जून, 1936 को अबीसीनिया से भाग कर आए सम्राट हेलीसिलेसी ने स्वयं राष्ट्रसंघ की असेम्बली की बैठक में उपस्थित होकर इटली के बर्बरतापूर्ण दुष्कृत्यों का रोमांचकारी वर्णन किया तथा राष्ट्रसंघ के सदस्यों से सहायता की प्रार्थना की। किन्तु राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य पर हेलीसिलेसी की प्रार्थना को कोई प्रभाव नहीं पङा।
केवल रूस ने अबीसीनिया के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये उसका समर्थन किया, किन्तु रूस की सभी माँगों को अस्वीकार करते हुये 15 जुलाई को इटली के विरुद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा लिये गये। फ्रांस और ब्रिटेन के प्रयास से अबीसीनिया को राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया।
नवम्बर, 1938 में ब्रिटेन और फ्रांस ने अबीसीनिया पर इटली के आधिपत्य को मान्यता देते हुए राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धांतों को तलांजली दे दी। केवल 19 महीनों के बाद मुसोलिनी ने दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके इस मान्यता का समुचित उत्तर दे दिया।
अबीसीनिया युद्ध के परिणाम
अबीसीनिया युद्ध, दो विश्व युद्धों के बीच के काल की महत्त्वपूर्ण घटना थी। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस युद्ध के अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले।इसने राष्ट्रसंघ की निर्बलता को प्रदर्शित कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ प्रबल राष्टों के आक्रमण से छोटे और निर्बल राष्ट्रों की रक्षा करने में असमर्थ है।
अतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध से इटली और जर्मनी की घनिष्ठता बढने लगी, क्योंकि इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के बाद जर्मनी ने शस्त्र देकर इटली की संकटमय स्थिति में सहायता की थी। राष्ट्रसंघ की निर्बलता से लाभ उठाकर हिटलर ने वर्साय संधि तथा लोकार्नो संधि को भंग कर राइन प्रदेश में किलेबंदी आरंभ कर दी। स्पेन के गृह युद्ध में जर्मनी और इटली ने खुलकर हस्तक्षेप किया।
हिटलर ने आस्ट्रिया का अपहरण कर लिया, चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग कर दिया और अंत में पोलैण्ड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्वयुद्ध का श्रीगणेश कर दिया। अबीसीनिया युद्ध में मुसोलिनी की सफलता के कारण उसके सिर पर लगे लोकप्रियता के मुकुट में ख्याति एवं लोकप्रियता की एक और पंखुङी लग गई।
राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया तथा उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए। यद्यपि राष्ट्रसंघ की इन कार्यवाहियों का इटली पर कोई प्रभाव नहीं पङा, किन्तु इटली ने राष्ट्रसंघ से अपना संबंध विच्छेद कर लिया।
रोम-बर्लिन-धुरी
अबीसीनिया युद्ध के अवसर पर इटली इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस से अत्यधिक नाराज हुआ। इस संकट के समय हिटलर आदि से अंत तक तटस्थ रहा तथा इटली को अस्र – शस्रों से सहायता करता रहा। हिटलर की तटस्थता मुसोलिनी के लिये बहुत बङी नैतिक सहायता सिद्ध हुई । अतः जर्मनी की ओर उसका झुकाव स्वाभाविक था।
हिटलर और मुसोलिनी का मेल-मिलाप बढने लगा। फलतः 26 अक्टूबर, 1936 को इटली तथा जर्मनी के बीच एक समझौता हो या जो इतिहास में रोम-बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध है।इस समझौते में दोनों ने तय किया कि दोनों अपने समान हितों की पूर्ति के लिये समय-समय पर परस्पर वार्ता करेंगे, दोनों देश साम्यवाद का विरोध करेंगे और दोनों स्पेन की रक्षा करेंगे।
इस संधि के परिणामस्वरूप मुसोलिनी ने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर के आक्रमण का कोई विरोध नहीं किया।
स्पेन का गृह युद्ध
स्पेन गृह युद्ध यद्यपि उसकी आंतरिक स्थिति का विषय है, फिर भी इसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वाभिनय कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों के संगठन का आभास पहले ही मिल गया था। प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन तटस्थ रहा था। युद्ध के बाद एक भयंकर आर्थिक संकट आया जिससे बेकारी की समस्या गंभीर हो गयी।
मजदूरों में असंतोष बढ गया, हङतालें होने लगी और दंगे फसाद आरंभ हो गये। जनता सरकार के कुशासन से काफी परेशान थी। यद्यपि नाम के लिये वहाँ वैध राजसत्ता थी किन्तु वास्तव में वहाँ का राजा अलफान्सो पूर्णतः तानाशाह था। जनता में विद्रोह की भावना देखते हुये अलफान्सो ने रिवेरा नामक सेनापति की सहायता सले देश में सैनिक कानून लागू कर दिया
जिससे रिवेरा का स्वेच्छाचारी शासन आरंभ हो गया। 1923 से 1930 तक वह अपना स्वेच्छाचारी शासन करता रहा, किन्तु देश में दंगे, विद्रोह और हङतालें होती रही। जन असंतोष को देखते हुये 1930 में रिवेरा ने पद त्याग कर दिया। उसके बाद अलफान्सो ने पुनः वैधानिक शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी।
किन्तु जनता विधान परिषद की माँग करने लगी और अलफान्सो इस माँग को टालता रहा। फलतः 1930 में वहाँ राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया और अलफान्सो स्पेन छोङकर भाग गया। इसके बाद स्पेन में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई।
गणतंत्र स्थापित होने के बाद वहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिये विभिन्न दलों में संघर्ष होने लगा। 1936 के आम चुनावों में उदार तथा अनुदार दोनों दलों को प्रायः बराबर स्थान प्राप्त हुए। जब उदार दल ने सत्ता अपने हाथ में लेनी चाही तो जनरल फ्रेंको के नेतृत्व में 18 जुलाई, 1936 को अनुदार दल ने गृह-युद्ध आरंभ कर दिया।
संपूर्ण स्पेन में एकाएक गृह युद्ध की आग भङक उठी। सैनिक अधिकारियों द्वारा निर्देशित यह गृह युद्ध पूर्णतया योजनाबद्ध था और इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। जनरल फ्रेंको ने विदेशी शक्तियों से सहायता माँगी। जर्मनी और इटली यह समझते थे कि स्पेन में यदि उनके जैसी (अधिनायकवादी) शासन प्रणाली स्थापित हो जाय तो उसकी सहानुभूति सदा उनके साथ रहेगी।
अतः उन्होंने जनरल फ्रेंको को सहायता देना अपना कर्त्तव्य समझा। किन्तु फासिस्टवाद के विरुद्ध गणतंत्र को मदद देना रूस ने अपना कर्त्तव्य समझा। किन्तु फासिस्टवाद के विरुद्ध गणतंत्र को मदद देना रूस ने अपना कर्त्तव्य समझा। किन्तु उस समय रूस उतना शक्तशाली नहीं था तथा रूस और स्पेन की सीमाएँ मिली-जुली नहीं थी।
अतः स्पेन के गणतांत्रिक सरकार को उश मात्रा में मदद नहीं कर सका जिस मात्रा में फ्रेंको को हिटलर और मुसोलिनी से सहायता प्राप्त हो रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन को यह भय था कि कहीं यह गृह युद्ध यूरोपीय विश्व युद्ध में परिवर्तित न हो जाय, क्योंकि फासिस्ट देश फ्रेंको की सफलता के लिये कटिबद्ध थे और यदि दूसरे देशों ने इसका विरोध किया तो विश्व युद्ध का हो जाना असंभव नहीं था।
अतः ब्रिटेन और फ्रांस तटस्थता का ढोल पीटकर खामोश बैठे रहे। फलस्वरूप इटली तथा जर्मनी की सहायता से जनरल फ्रेंको को विजय प्राप्त हो गहयी। 28 मार्च, 1939 को स्पेन की राजधानी मेड्रिड का पतन हो गया और गृह-युद्ध भी समाप्त हो गया। स्पेन में जनरल फ्रेंको की तानाशाही स्थापित हो गयी।
युद्ध के परिणाम
यद्यपि यह युद्ध स्पेन का आंतरिक मामाला था किन्तु विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हो गया। इस युद्ध ने इटली व जर्मनी की मित्रता को प्रगाढ बना दिया, जर्मनी तथा जापान के साथ इटली भी एण्टी-कॉमिण्टर्न पैक्ट में सम्मिलित हो गया और यूरोप में फासिस्ट शक्तियों की स्थिति मजबूत हो गयी।
हिटलर और मुसोलिनी को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस साम्यवाद के हौवे से बुरी तरह आशंकित हैं और उन्हें यह भय दिखाकर कुछ भी कराया जा सकता है। इससे उन्हें यह ज्ञान हो गया कि उनके आक्रमणों को रोकने का साहस पश्चिमी लोकतंत्र में नहीं है।
राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा योजना अंतिम रूप से विफल हो गयी। स्पेन की सरकार ने इस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाने का कई बार प्रयत्न किया, किन्तु संघ की असेम्बली ने केवल 2 अक्टूबर, 1937 को यह प्रस्ताव पास किया कि स्पेन से हट जाना चाहिये। किन्तु जर्मनी और इटली अपने स्वयंसेवक हटाने के लिये तैयार नहीं थे।
अतः राष्ट्रसंघ अपने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं कर सका। शूमैन ने तो यहाँ तक लिखा है कि इंग्लैण्ड और फ्रांस ने अहस्तक्षेप की नीति के आधार पर तथा अमेरिका ने तटस्थता के नाम पर स्पेन को शस्त्र बेचना और भेजना बंदर कर दिया और इस प्रकार धुरी राष्ट्रों द्वारा स्पेन के लोकतंत्र की हत्या में सहयोग दिया गाय।इस युद्ध ने धुरी राष्ट्रों को ब्रिटेन और फ्रांस पर धौंस जमाने और अधिक रियायतें प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। इसके अलावा इस गृह युद्ध में जर्मनी को लङने के नए तरीकों का प्रयोग करने का अवसर मिल गया।
सज्जन समझौता
इंग्लैण्ड, इटली को मित्र बनाने के लिये प्रयत्नशील था। अतः 2 जनवरी, 1937 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में सज्जन समझौता कहते हैं। इसमें दोनों ने स्पेन की तटस्थता और अखंडता को स्वीकार किया और भूमध्यसागर में गुजरने की स्वाधीनता के सिद्धांत को मान्यता दी।
किन्तु इसके बाद मुसोलिनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध प्रबल प्रचार आरंभ कर दिया। उसने अपनी नौ सेना बढाने की विशाल योजना की घोषणा की, जिससे इंग्लैण्ड का भयभीत होना स्वाभाविक ही था। जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया का अपहरण किया गया, किन्तु मुसोलिनी ने इसका विरोध नहीं किया।
चेकोस्लोवाकिया के संकट के समय मुसोलिनी ने हिटलर को म्यूनिख समझौते के लिये तैयार किया। इस समय ब्रिटेन इटली को संतुष्ट करने तथा उसे हिटलर से पृथक रखने का प्रयत्न कर रहा था। फलतः 16 नवम्बर, 1939 को ब्रिटिश-इटालियन पैक्ट हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने अबीसीनिया पर इटली की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की।
इसके बदले में इटली ने स्पेनिश प्रदेश में युद्ध की समाप्ति पर अपने स्वयंसेवक हटाने तथा निकट पूर्व में ब्रिटिश विरोधी प्रचार ने करने का आश्वासन दिया।
फौलादी समझौता
फ्रांस ने भी अबीसीनिया पर इटली के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, किन्तु इटली की संसद में फ्रांस से कोर्सिका तथा ट्यूनिसिया लेने की प्रबल माँग की गयी। इससे फ्रांस और इटली का वैमनस्य बढने लगा। अतः इटली ने 22 मई, 1939 को जर्मनी के साथ एक राजनैतिक और सैनिक समझौता किया।
इसी समझौते को फौलादी समझौता कहते हैं। क्योंकि इसमें दोनों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया था। इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि उस पर जर्मनी की अपेक्षा ब्रिटेन और फ्रांस अधिक सुगमता से आक्रमण कर सकते थे और वह जर्मनी की तुलना में अभी निर्बल भी था। अतः मुसोलिनी ने युद्ध का समर्थक होते हुये भी पोलैण्ड के मामले में शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास किया।
मुसोलिनी का अंत
मुसोलिनी के प्रयासों के बावजूद जब हिटलर ने 1 सितंबर, 1939 को पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया तो फौलादी समझौते के विपरीत वह तटस्थ रहा। वह युद्ध में कूदने के लिये अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। इटली के लिये आक्रमण करने और युद्ध में कूदने के लिये उपयुक्त अवसर वहीं था, जबकि मित्र राष्ट्रों की पराजय लगभग निश्चित हो चुकी थी, किन्तु उन्होंने आत्मसमर्पण न किया हो।
अतः हिटलर ने जब फ्रांस को लगभग परास्त कर दिया तब 10 जून, 1940 को इल डूचे ने हर्षोन्मत्त जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भाग्य द्वारा निश्चित की गयी घङी आ पहुँची है। हम समुद्र में बाँधने वाली प्रादेशिक और सैनिक श्रृंखलाओं को तोङना चाहते हैं।
हम अवश्य ही विजयी होंगे ताकि इटली में, यूरोप में और विश्व – शांति स्थापित हो सके। 11 जून, 1940 को इटली ने ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कौन जानता था कि इस युद्ध में मुसोलिनी की न केवल हार होगी अपितु उसके स्वदेशवासी उससे रुष्ट होकर 28 अप्रैल, 1945 को उसे उसकी प्रेयसी सहित गोली मारकर मार डाला गया।

1. पुस्तक- आधुनिक विश्व का इतिहास (1500-1945ई.), लेखक - कालूराम शर्मा
Online References wikipedia : मुसोलिनी की विदेश नीति