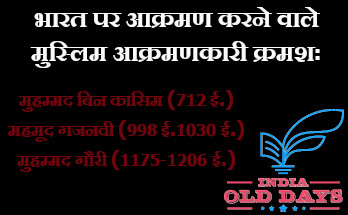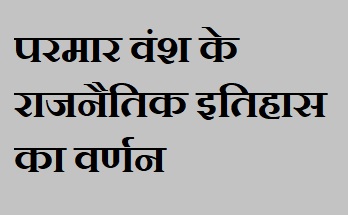1500 ई.पू. से 600 ई.पू. के काल खंड को वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है।इस काल में वेदों की रचना की गयी थी।
वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है-
- ऋग्वैदिक काल – 1500-1000 ई.पू.
- उत्तर वैदिक काल – 1000-600 ई.पू.
यहां पर हम ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.) के बारे में आपको बतायेंगे-
अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचना 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. के मध्य तथा अन्य वेदों की रचना इसके बाद मानते हैं। जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है।
ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है।
ऋग्वेद में आर्यों के निवास-स्थल के लिये सर्वत्र सप्त सिन्धवः शब्द का प्रयोग मिलता है।
ऋग्वेद में यमुना का प्रयोग तीन बार तथा गंगा का प्रयोग एक बार हुआ है।
राजा का पद वंशानुगत होता था।
आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
राजा के ऊपर जनता (विश) का अंकुश रहता था।
राजकीय कार्यों में राजा की सहायता के लिये अनेक पदाधिकारी थे, जिनमें सेनापति तथा पुरोहित को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।
ग्रामणी ग्राम का मुखिया कहलाता था।
ऋग्वैदिक काल में पुत्र की भाँति पुत्री का उपनयन संस्कार होता था।
वह अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुयी अध्ययन करती थी।
ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिनमें घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, निवावरी, पौलोमी, काक्षावृती और विश्ववारा आदि मुख्य थी। इन्होंने ऋषियों की भाँति ही ऋचाओं की रचना की।
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार भी प्राप्त था।
ऋग्वैदिक काल में संगीत के अलावा घुङदौङ, रथ दौङ तथा मल्ल युद्ध मनोरंजन के अन्य साधन थे।
ऋग्वेद के 7 वें मंडल में सुदास एवं दस राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि परुष्णी (रावी)नदी के तट पर लङा गया, इस युद्ध में सुदास की विजय हुई।
संपूर्ण आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। ये जन ग्रामों में निवास करते थे। समाज की इकाई परिवार थी।
सबसे वृद्ध व्यक्ति ही परिवार का स्वामी होता था, जिसे कुलप कहा जाता था।
ऋग्वैदिक काल में विवाह एक उच्च एवं पवित्र संस्कार माना जाता था।
याज्ञिक कार्यों में पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी।
ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं, जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी।ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था।
YouTube Video
ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री संतान प्राप्ति के लिये अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। ऋग्वेद में कपङे के लिये वस्त्र, वास और वसन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।
इन्द्र अत्यधिक शक्तिशाली और पराक्रमी देवता थे, जो दस्युओं के विजेता थे। वे आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता थे।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बङा महत्त्व है।आर्य निवास की यह अति महत्त्वपूर्ण नदी थी।
राजकर के रूप में पशु और अन्न दोनों ही दिये जा सकते थे।
ऋग्वैदिक काल में वस्तु के बदले वस्तु की विनिमय प्रथा का प्रचलन था।
व्यापार के लिये दूर देशों तक व्यापार करने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था।
ऋग्वेद में भिषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है।इस काल में चमङे का कार्य करने वाले चर्म्मन कहलाते थे।
ऋग्वेद काल में अयस का प्रयोग कवच शिरस्त्राण, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र-शस्त्र के बनाने में होने लगा।
ऋग्वेद में सूत, रथकार और कर्मार नाम उल्लिखित हैं, जो राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे।
आर्य धातु गलाने और पीटकर विभिन्न आकार देने में पारंगत थे।
स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता था, जो जनता की गतिविधियों की सूचना राजा को देते रहते थे।
ऋग्वेद में हिरण्यपिण्ड का वर्णन मिलता है।निष्क, आभूषण आदि हिरण्यपिण्ड से ही बनाये जाते थे।
ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था।
सभा-समिति राजा को उसके दैनिक प्रशासन और न्यायिक अधिकार से युक्त थी।इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था।
ऋग्वेद में तक्षन् अथवा त्वष्ट्रा का वर्णन मिलता है।यह लकङी का कार्य करता था। यह मुख्यतः रथ का निर्माण करता था।
इस काल के प्रमुख देवता पूषन पशुओं का देवता, सूर्य ही शक्ति का परिचायक थे, जो औषधि और वनस्पति जगत के सम्वर्द्धन में योग करते थे।
अग्नि देवता का महत्त्व इन्द्र के बाद प्रमुख थी। अग्नि को ऋग्वेद में आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृत पृष्ठ, घृत-लोम, अर्चिलोम या वभ्रलोम कहा गया है।
विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता तथा ऋग्वेद में आकाश का विचरण करने वाले सूर्य का रूप थे।
ऋग्वेद में 33 देवी-देवताओं का उल्लेख मिलता है।
‘असतो मा सद् गमय’ वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है।
मरुत रुद्र के पुत्र थे, इसलिये वे अपने पिता की ही तरह भयंकर थे। वे आँधी व तूफान के देवता थे।
सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को सम्बोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही उल्लेखित है।
घौ सबसे प्राचीन एवं आकाशीय देवता थे।
ऋग्वैदिक काल में विष्णु को उऊगाय के नाम से भी जाना जाता था।
ऋग्वेद के 9 वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में सोम को सूर्या का पति कहा गया है।
ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक हैं, वह देवता सोम है।
आश्विन का वर्णन ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है। आश्विनों को नासत्या (अश्विनी कुमार)भी कहा गया है। ये देवता पीङा निवारक एवं विपत्तियों को हराने वाले देवता होते थे।
ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था।
ऋग्वेद के 9 वें मंडल में सोम (आर्य सुरा पीते थे। सुरा के साथ-साथ आर्य समाज में एक पेय पदार्थ होता था, जिसे सोम रस कहा जाता था।)की प्रशंसा की गयी है।
इन्द्र आँधी-तूफान, बिजली और वर्षा के देवता थे। इस काल में इन्द्र ही सर्वमान्य देवता थे और सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माने जाते थे।इन्द्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं।
इस काल में स्त्री-पुरुष समान रूप से आभूषण पहनते थे। इस काल में गाय का अवधा (जिसका हत्या न की जा सके)माना जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था।
आर्य समाज में घोङा (अश्व) परम पशुओं में कुत्ता, सुअर, गधा तथा हिरण प्रमुख थे।
अग्नि मनुष्य और देवता के मध्य सेतु के रूप में विद्यमान है।
वरुण का तीसरा स्थान है, जो जल या समुद्र का देवता, पृथ्वी व सूर्य का निर्माता है तथा ऋतु अर्थात् प्राकृतिक सन्तुलन की रक्षा करता है, इसे ऋतस्य गोप कहा जाता है।