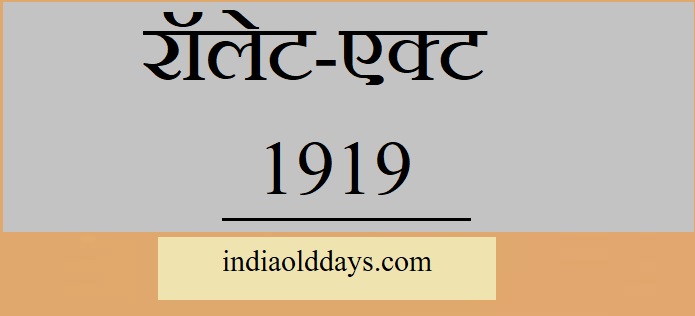चित्तौङ और दिल्ली सल्तनत का इतिहास
चित्तौङ और दिल्ली सल्तनत – समरसिंह के उत्तराधिकारी रत्नसिंह के समय में मुसलमानों ने चित्तौङ को जीत लिया था।
रत्नसिंह और अलाउद्दीन खिलजी –रावल समरसिंह के बाद 1302 ई. में रत्नसिंह गुहिलों के सिंहासन पर बैठा। वह समरसिंह का पुत्र था। एक साल बाद ही मेवाङ राज्य को सर्वाधिक खतरनाक अभियान का सामना करना पङा जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुहिलों के राज्य को पूरी तरह से पदाक्रान्त करके उसकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया।
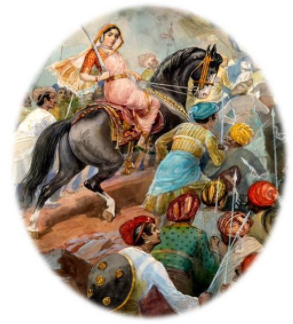
अलाउद्दीन के चित्तौङ आक्रमण के कारण – समरसिंह सुल्तान की सेना को गुजरात विजय करने का मार्ग देकर थोङे समय के लिये चित्तौङ को सुरक्षित रखने में सफल रहा था परंतु उसके पुत्र को सुल्तान के आक्रमण का सामना करना पङा। अलाउद्दीन ने चित्तौङ पर आक्रमण किस उद्देश्य से प्रेरित होकर किया, इस संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। अलाउद्दीन के चित्तौङ आक्रमण के मुख्य कारण इस प्रकार बताये जा सकते हैं-
अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा
इतिहासकार बरनी ने लिखा है कि अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में मिलने वाली सफलताओं ने अलाउद्दीन को अहंकारी बना दिया और वह सिकंदर महान की भाँति विश्वविजय की आकांक्षा रखने लगा। परंतु दिल्ली कोतवाल एवं उसके वृद्ध सलाहकार मलिक अल्लाउल्मुल्क ने उसे सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के पूर्व पहले संपूर्ण हिन्दुस्तान को जीतना चाहिये।
इसके बाद देश के बाहर साम्राज्य विस्तार की योजना बनाना तथा उस पर अमल करना अधिक उचित होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को उसका सुझाव पसंद आ गया और उसने संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित करने का दृढ निश्चय कर लिया।
इसी अभिप्राय से उसने भारत के सुदूर प्रांतों में अपनी सेनाओं को भेजा था जिनकी शानदार विजयों के कारण बंगाल, सिन्ध, गुजरात, मालवा, पंजाब, काश्मीर आदि राज्य उसके साम्राज्य के अंग बना लिये गये । वह सुदूर दक्षिण को भी अपने राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत रखना चाहता था।
दक्षिण-भारत की विजय और उत्तरी भारत पर अपने अधिकार को स्थायी बनाये रखने के लिये सल्तनत के पङौसी राजस्थान के स्वतंत्र राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था। इसलिए उसने रणथंभौर, सिवाना, जालौर आदि पर आक्रमण किये थे। चित्तौङ पर उसका आक्रमण इसी नीति का एक अंग था।
मेवाङ का बढता हुआ प्रभाव
जैत्रसिंह, तेजसिंह और समरसिंह जैसे योग्य एवं पराक्रमी गुहिल वंशी राजाओं के शासनकाल में मेवाङ की नवोदित शक्ति के विकास के साथ-साथ मेवाङ राज्य की सीमाओं का भी विस्तार होता जा रहा था। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के सैनिक अभियान भी गुहिलों की शक्ति को अधिक क्षति नहीं पहुँचा पाये और इससे उनका आत्म विश्वास तथा साहस बढा। मेवाङ के सैनिकों में नया उत्साह पैदा हुआ।
मेवाङ के शासकों ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुये आसपास के क्षेत्रों को जीतकर गुजरात में अपना प्रभाव बढाने का प्रयास किया। मालवा के कुछ क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव कायम हो गया। 1299 ई. में रावल समरसिंह ने गुजरात पर आक्रमण करने जा रही शाही सेना के साथ सहयोग न करके उल्टे उससे दंड वसूल करके आगे जाने दिया।
अलाउद्दीन इस घटना को विस्मृत नहीं कर पाया और अवसर मिलते ही चित्तौङ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया।
चित्तौङ दुर्ग का सामरिक महत्त्व
अलाउद्दीन के आक्रमण का एक कारण चित्तौङ दुर्ग का सामरिक महत्त्व तथा भौगोलिक स्थिति भी था। चित्तौङ का दुर्ग समुद्र की सतह से 1850 फुट ऊँचाई पर स्थित है। आसपास के चौरस मैदान से इसकी ऊँचाई 500 फुट है। यह लगभग 3 मील लंबी और आधा मील चौङी पहाङी पर स्थित है। मुख्य दुर्ग पर चारों तरफ से मजबूत सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है।
सुरक्षा दीवार में तीर चलाने के लिये बङे-बङे छिद्र भी बने हुए हैं। मौर्य वंशी राजा चित्रांग द्वारा निर्मित यह दुर्ग अपनी अभेद्यता के लिये विख्यात रहा है। मुस्लिम सेनाएँ अभी इस दुर्ग को जीतने में असफल रही थी। अलाउद्दीन जैसे सुल्तान के लिये चित्तौङ की स्वतंत्रता एक खुली चुनौती थी।
इसके अलावा चित्तौङ की भौगोलिक स्थिति भी काफी महत्त्वपूर्ण थी। दिल्ली से मालवा,गुजरात तथा दक्षिण-भारत जाने वाला मार्ग इसी के पास होकर गुजरता था। मालवा-गुजरात और दक्षिण-भारत को अपने राजनातिक प्रभाव के अन्तर्गत रखने वाले किसी भी दिल्ली सुल्तान के लिए चित्तौङ को अपने अधिकार में बनाये रखना जरुरी था, ताकि उसकी सेनाओं को किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करना पङे। इस दृष्टि से भी अलाउद्दीन के लिये चित्तौङ जीतना आवश्यक था।
पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा
कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन, चित्तौङ के राजा रत्नसिंह की विख्यात सुन्दर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा रखता था और उसे प्राप्त करने के लिये ही उसने चित्तौङ पर आक्रमण किया था। परंतु बहुत से अन्य इतिहासकार इसे आधारहीन बताते हैं।
अलाउद्दीन का आक्रमण
रणथंभौर की विजय के बाद सुल्तान अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ चित्तौङ पर आक्रमण करने के लिये चल पङा। इस अभियान में उसके साथ सुप्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो भी चला। खुसरो के द्वारा हमें इस आक्रमण से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है।
वह लिखता है कि सुल्तान ने 28 जनवरी, 1303 ई. को सेना सहित दिल्ली से प्रस्थान किया। परंतु न तो खुसरो ने और न ही किसी अन्य मुस्लिम इतिहासकार ने सुल्तान द्वारा तय किये गये मार्ग का विवरण दिया है। अमीर खुसरो केवल इतना ही लिखता है कि चित्तौङ के समीप पहुँचने पर सुल्तान ने गंभीरी और बेङच नदी के मध्य शाही शिविर स्थापित करने के आदेश दिये।
अलाउद्दीन ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया और दोनों दिशाओं से दुर्ग को घेरने का काम शुरू कर दिया। सुल्तान ने स्वयं अपना शिविर चित्तौङी नामक टेकरी पर लगाया, जहाँ से वह घेराबंदी के कार्य का निरीक्षण करता था और वहीं दरबार लगाता था। खुसरो लिखता है कि दो महीनों की निरंतर घेराबंदी के बाद भी कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला।
चित्तौङ पर इस समय रावल रत्नसिंह का शासन था। वह 1302 ई. में ही चित्तौङ का शासक बना था। अमीर खुसरो ने यद्यपि चित्तौङ के शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया, तथापि वह लिखता है कि चित्तौङ का राणा समस्त हिन्दू शासकों में श्रेष्ठ था और हिन्दूस्तान के सभी शासक उसकी श्रेष्ठता को मानते हैं। चित्तौङ दुर्ग के बारे में भी खुसरो ने विस्तार से लिखा है।
राणा रत्नसिंह ने अपने सरदारों एवं सैनिकों के साथ शाही सेना को मुँह तोङ जवाब दिया और दो महीने तक शाही सेना कोई सफलता अर्जित नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और अब उसने नियमित रूप से दुर्ग की दीवारों के आसपास तक धावे मारने का क्रम शुरू किया।
इसके साथ ही ऊँचे-ऊँचे चबूतरों का निर्माण करवाया गया और उन चबूतरों पर पत्थर तथा प्रक्षेपास्र फेंकने वाले यंत्र लगवाये गये। इनकी सहायता से किले की दीवारों पर भारी-भारी पत्थर फेंके जाते रहे परंतु इन पत्थरों के प्रहारों से किले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा। यह सिलसिला आठ महीने तक चलता रहा।
राजपूत किले के परकोटों से मार्चा बनाकर शाही सेना का मुकाबला करते रहे। कुम्भलगढ शिलालेखों से पता चलता है कि इस अवधि में सीसोदे का सामन्त लक्ष्मणसिंह अपने सात पुत्रों सहित किले की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था।
चित्तौङ दुर्ग का घेरा लंबे समय तक चला।इससे यह स्पष्ट हो जाा है कि राणा रत्नसिंह एवं उसके सरदारों ने अंतिम क्षण तक शत्रु से संघर्ष करने का दृढ निश्चय कर रखा था। चित्तौङ की इस संकटप्रद स्थिति में राजस्थान के अन्य हिन्दू सरदारों ने रत्नसिंह की किस प्रकार से सहायता की अथवा वे उदासीन बने रहे, यह कहना कठिन है।
इस संंबंध में डॉ.के.एस.लाल ने लिखा है कि, अनवरत प्रतिद्वंद्विताओं और राजपूताना की रियासतों की एक दूसरे के प्रति घोर उदासीनता को दृष्टिगत रखते हुये यह सरलता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चित्तौङ के नवारूढ शासक को अकेले लङना पङा।
जब चारों ओर सर्वनाश के चिह्न दिखाई देने लगे और शत्रुओं से बचने तथा दुर्ग की रक्षा की आशा न रही तो अपनी स्रियों का सतीत्व बचाने के लिये जौहर रचाया गया और राजपूती परंपरा का पालन करते हुये राजपूत महिलाओं और बच्चों को धधकती हुई अग्नि में अर्पण कर दिया गया।
कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रन्थ में जौहर के दृश्य का ह्रदय विदारक उल्लेख करते हुये लिखा है कि सुन्दरी पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया, जिसमें समस्त नारी-सौन्दर्य एवं यौवन सम्मिलित था, जिसका तातारों की काम पिपासा द्वारा लांछित होने का भय था। इनको तहखाने में ले जाया गया और भस्भीभूत करने वाला तत्व (अग्नि) में अपमान से त्राण पाने के लिये भीतर छोङकर, द्वार बंद कर दिया गया।
इसके बाद राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर किले के फाटक खोल दिये और मुस्लिम सेना पर टूट पङे और लङते-लङते वीरगति को प्राप्त हुए। शाही सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो ने लिखा है कि घमासान युद्ध के बाद 25 अगस्त, 1303 को किला फतह हुआ।
दूसरे दिन क्रुद्ध सुल्तान ने चित्तौङ की आम जनता के कत्लेआम का आदेश दे दिया। ऐसा अनुमान है कि लगभग 30,000 निर्दोष एवं असहाय लोगों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही दुर्ग के भव्य मंदिरों तथा भवनों को भी नष्ट किया गया। मुस्लिम सैनिकों ने भी जी भर कर लूट-खसोट की।
सुल्तान कुछ दिन चित्तौङ में रहकर वापस दिल्ली लौट गया। जाने के पूर्व चित्तौङ का दुर्ग और मेवाङ राज्य अपने बङे पुत्र खिज्रखाँ को सौंप दिया और चित्तौङ का नाम बदल कर अपने पुत्र के नाम पर खिज्राबाद कर दिया।
चित्तौङ नरेश रत्नसिंह के भाग्य तथा अंत के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं हैं। इस अभियान में उपस्थित अमीर खुसरो लिखता है कि राव पहले भाग गया परंतु पीछे से स्वयं शरण में आया और तलवार की बिजली से बच गया। इससे लगता है कि उसे जीवनदान मिल गया। नैणसी का मत है कि रत्नसिंह लङते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ।
जैनग्रंथ नाभिन्दन-जिनोधार-प्रबंध के अनुसार चित्तौङ नरेश पकङा गया और उसे एक नगर से दूसरे नगर बंदर की भाँति घुमाया गया। परंतु अमीर खुसरो और जैन ग्रन्थ – दोनों ही उसके अंत के बारे में चुप हैं। इस प्रकार के विवरणों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं।
डॉ. गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं यदि इसमें सत्य का अंश है तो अलाउद्दीन का चित्तौङ के किले पर आना और रत्नसिंह को छल से बंदी बनाने की संपूर्ण कथा का तारतम्य बैठ जाता है। परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि राणा रत्नसिंह लङते हुये वीरगति को प्राप्त हुआ होगा।
खिज्रखाँ कुछ वर्षों तक चित्तौङ में रहा। उसे गुहिल वंश की छोटी शाखा सीसोदा के सामंत ने चैन से नहीं बैठने दिया। परिणामस्वरूप अलाउद्दीन ने खिज्रखाँ को वापिस बुला लिया और चित्तौङ का दुर्ग तथा मेवाङ का राज्य जालौर के चौहान शासक कान्हङदेव के भाई मालदेव को सौंप दिया।
कहा जाता है कि जालौर अभियान के समय एक अवसर पर मालदेव ने अलाउद्दीन की प्राणरक्षा की थी। जालौर के पतन के बाद मालदेव सुल्तान की सेवा में चला गया और अब सुल्तान ने कृतज्ञतावश उसे अपनी तरफ से चित्तौङ का प्रान्तपति नियुक्त कर दिया।
परंतु चित्तौङ के स्वाभिमानी राजपूतों को यह पसंद नहीं आया और वे अपने सीमित साधनों के बाद भी मालदेव को परेशान करते रहे। सीसोदा के सामंत हम्मीर ने मालदेव को सबसे अधिक परेशान कर रखा था। यह वही हम्मीर था जिसका दादा लक्ष्मणसिंह अपने सात पुत्रों सहित चित्तौङ दुर्ग की घेराबंदी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था। हम्मीर ने मालदेव के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।
मालदेव ने अनपी पुत्री का उसके साथ विवाह करके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1321 ई. के आसपास मालदेव की मृत्यु हो गयी और उसके कुछ समय बाद ही हम्मीर ने संपूर्ण मेवाङ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
References : 1. पुस्तक - राजस्थान का इतिहास, लेखक- शर्मा व्यास

Online References wikipedia : चित्तौङ और दिल्ली सल्तनत