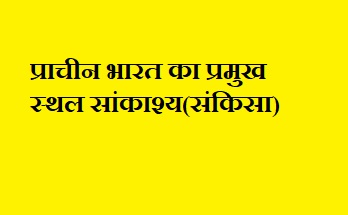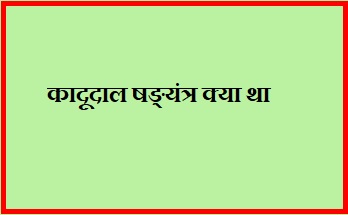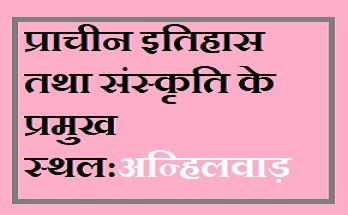मध्यकालीन भारत में कर अधिकारी तथा संग्रहकर्ता
कर अधिकारी तथा संग्रहकर्ता
आमिल
मध्यकाल तथा ब्रिटिश काल के प्रारंभ में कर संग्रहकर्ताओं का समान नाम था।
देसाई अथवा देशमुख
पश्चिम भारत तथा दक्कन में जिला (सरकार)अथवा उपजिला (परगना) स्तर पर वंशानुगत मख्य कर अधिकारी को कहा जाता था।
देशपांडे
पश्चिम भारत तथा दक्कन में जिला तथा उपजिला स्तर पर कर संग्रहण का वंशानुगत लेखाकार को देशपांडे कहा जाता था।
इजारदार
पूर्वी भरत का कर कृषक
इक्तादार
दिल्ली सल्तनत काल के दौरान इक्ता धारका, इन्हें मुक्ति भी कहा जाता था।
जागीरदार
मुगलों के काल में जागीर धारक
कुलकर्णी
पश्चिम भारत तथा दक्कन में ग्रामीण लेखाकार
मालगुजार
अंग्रेजों के काल में उत्तर भारत तथा मध्य भारत में मालगुजारी, अर्थात् कर अधिकार, धारका
मामलदार
मराठों के अधीन पश्चिम भारत तथा दक्कन में जिला तथा उपजिला स्तर पर गैर वंशानुगत कर अधिकारी।
मुकद्दम
उत्तर भारत के ग्राम प्रधान, इन्हें खोत भी कहा जाता था।
पालेगर अथवा पोलीगर
दक्षिण भारत में कर संग्रहण का वंशानुगत अधिकार रखने वाला जमींदार।
पटेल अथवा पाटिल
पश्चिम भारत तथा दक्कन के ग्राम प्रधान।
पटवारी
उत्तर तथा मध्य भारत के ग्रामीण लेखाकार।
ठीकादार
ब्रिटिश काल में पूर्वी भारत के बङे जमींदार से जमीन का ठीका प्राप्त करने वाले।
विभिन्न कर
अबवाब
जमींदारों तथा जन अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर।
चौथ
मुगलों तथा स्थानीय शासकों द्वारा अपरिभाषित भूमि क्षेत्र पर भूमिकर का एक चौथाई भाग जो मराठों को दिया जाता था ताकि मराठा सैनिक उन क्षेत्रों पर आक्रमण न करें।
जिज्या
इस्लामी राज्य में जिम्मी (गैर-मुस्लिमों) द्वारा सरकार को दिया जाने वाला धार्मिक कर।
खराज
मध्यकालीन भारत के मुस्लिम शासित क्षेत्रों में भूमि कर।
खम्श
परंपरागत रूप से लूट, गङे खजाने, खान आदि में से राज्य द्वारा लिया जाने वाला पांचवां भाग जो अलाउद्दीन खिलजी के काल से पांच में से चार भाग हो गया।
सैर अथवा सयीर
भूमिकर के अलावा कर, मुख्यतः पारगमन कर।
सरदेशमुखी
दस प्रतिशत का अतिरिक्त कर जो वंशानुगत अधिकारों का दावा करते हुए मराठा शासक महाराष्ट्र क्षेत्र से लेते थे।
जकात
इस्लामी राज्य में धनी मुसलमानों द्वारा अपने गरीब भाइयों के निर्वाह के लिये दिया जाने वाला एक धार्मिक कर।
कृषि में संलग्न वर्ग
बरगदार
पूर्वी भारत के बटाईदार। भू-स्वामी जब चाहे तब उन्हें जमीन से बेदखल कर सकता था।
भागदार
पश्चिम भारत के कुछ भागों में एक संयुक्त गांव का हिस्सेदार । इन्हें पाटीदार तथा नरवादार भी कहा जाता था।
ग्रंतिदार
पूर्वी भारत के कुछ भागों (जैसे कि जैसोर जिला)में सीधे सरकार अथवा जमींदार के अधीन भूमिधारक (ग्रंति)। पूर्वी भारत के अन्य भागों में इस प्रकार के भूमिधारकों के कई नाम थे – रंगपुर जिले में जोतदार, बाकरगंज जिले में हवलदार, पुर्णिया जिले में गचदार तथा मिदनापुर जिला में मंडल। ये लोग अधिकतर बङे भूमिधारक थे तथा अपनी भूमि पर खेती करवाने के लिये भाङे के मजदूरों पर निर्भर थे। इनकी उत्पत्ति का कारण मुख्यतः ब्रिटिश काल में बेकार भूमि को बङे पैमाने पर खेती के अधीन लाने से था।
हली अथवा हलिया
पश्चिम भारत के बंधुआ कृषि मजदूर।
कमिया
पूर्वी भारत के बंधुआ कृषि मजदूर।
कनमदार
केरल में जमींदारों (जेन्मी) के अधीन भूमिधारक। भूधारिता के दौरान (साधारणतः 12 वर्ष) कनमदार जेन्मियों को अन्य कृषकों से कम लगान देते थे। शुरू में उन्हें जेन्मियों को एक मोटी रकम (कनम) देनी पङती थी तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला लगान उसी हिसाब से कम किया जाता था। कनमदार या तो भूमि पर स्वयं खेती करते थे अथवा अन्य कृषकों, जैसे पट्टेदारों को दे देते थे।
खुदकाश्त
मुगलकालीन भारत के वैसे कृषक जिनका गांव में स्थायी निवास था, भूमि का स्वामित्व था, खेती के अपने उपकरण थे तथा जो सीधे राज्य को कर देते थे। महाराष्ट्र में इन्हें मिरासदार (मिरास के धारक) तथा राजस्थान में घरूहाला अथवा गवेति कहा जाता था।
कोर्फा
पूर्वी भारत में भूमि में कुछ विशेष प्रकार के अधिकार रखने वाले कृषक ।
मुजरियान
मुगलकालीन भारत का बटाईदार।
नत्तार
तमिलनाडु में स्थानीय भूमि तथा जनता पर प्रभाव रखने वाला स्थानीय शासक वर्ग का व्यक्ति ।
पाही
मुगलकालीन भारत का कृषक जो मूल रूप से बाहरी था लेकिन किसी गांव में या पङोस में रहकर दूसरे की भूमि पर खेती करता था। महाराष्ट्र में इन्हें ऊपरी कहा जाता था।
पटनीदार
पूर्वी भारत के कुछ भागों (जैसे कि बर्दवान जिला) में किसी जमींदारी में पटनी धारक।
व्यावसायिक प्रणालियां तथा प्रचलन
कार्टेज प्रणाली
यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत भारतीय जहाजों को, ऐसे स्थानों पर, जो कि पुर्तगालियों के लिये सुरक्षित नहीं थे, जाने के लिये तथा अपनी सामग्री को जब्त होने से बचाने के लिये गोवा के पुर्तगाली वायसराय से पास (कार्टेज) लेना पङता था।
दादनी प्रणाली
इस प्रणाली के अंतर्ग व्यवसायी (भारतीय तथा यूरोपीय) नकद तथा कच्चा माल अग्रिम (दादन) में शिल्पकारों को देते थे। तथा बाद में तैयार माल को खरीदते थे। हालांकि इसकी उत्पत्ति तथा विकास बंगाल में हुआ लेकिन बाद में इसका प्रसार भारत के अन्य भागों में भी हुआ। यह पुटिंग आउट प्रणाली की तरह नहीं था क्योंकि इस प्रणाली की खरीद-बिक्री में शिल्पकार को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी।
दामदुपाट
पश्चिम भारत में प्रचलित एक कानून जिसके अंतर्गत कोई भी कर्जदार ऋण की मूल रकम से अधिक ब्याज देने के लिये बाध्य नहीं था।
हुंडी
मुगलकाल में प्रचलित देशी विनिमय पत्र जिसमें एक खास समय के बाद (दो महीने या कम) भुगतान करने का वादा किया जाता था। भुगतान करने का वादा किया जाता था। भुगतान का यह वादा एक खास स्थान पर किया जाता था जिसमें, छूट, ब्याज, बीमा शुल्क तथा मुद्रा के स्थानांतरण की कीमत साथ होती थी। 18 वीं शताब्दी के दौरान हुंडी बङे व्यावसायिक लेन-देन का मानकीकृत माध्यम बन गया। लंबी दूरी के व्यापार में इससे न सिर्फ बढते हुए उधार की मांग को पूरा करने में मदद मिली बल्कि दूरस्थ स्थानों पर नकद रकम ले जाने में संलग्न खतरों से मुक्ति प्राप्त हो गई। यह व्यवसाय मुख्यतः पेशागत मुद्रा परिवर्तकों अथवा बैंकरों के हाथ में था जिन्हें सर्राफ कहा जाता था।
खतबंदी
एक अधिनियम जिसके द्वारा पूर्वी भारत के शिल्पकार 1770 के बाद अपना उत्पाद सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने के लिये बाध्य कर दिए गए।
व्यवसायी वर्ग
बनिया
पूरे उपमहाद्वीप में व्यवसायी। कुछ क्षेत्रों में ये बैंकरों तथा मुद्रा परिवर्तकों के रूप में भी कार्य करते थे।
बंजारा
पूरे भारत में कारवां व्यापार। खासकर अनाज, नमक तथा मवेशी का व्यापार करने वाले व्यवसायी।
चेट्टी अथवा चेट्टीयार
दक्षिण भारत के व्यवसायी।
गोलदार
गोला (गोदाम) वाले थोक व्यापारी।
महाजन
पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के थोक व्यापारी या बङे बैंकर।
मारवाङी
राजस्थान के मारवाङ के निवासी जो बैंकरों, व्यवसायियों अथवा दलालों का काम करते थे।
पैकार
व्यवसायियों के एजेंट जो पूर्वी भारत में शिल्पकारों का सामान खरीदते थे।
साहूकार
पश्चिम भारत के बैंकर तथा महाजन।
सौदागर
पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के बैंकर तथा महाजन।
सर्राफ
पेशागत बैंकर जो हुंडियों के द्वारा उधार देते थे।
विविध शब्दावली
औरांग
उत्पादित वस्तुओं का गोदाम अथवा स्थानीय निर्माण क्षेत्र
भाईचारा
भूमि अथवा अन्य संपत्ति पर सामूहिक अधिकार
बीघा
भूमि की माप जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं से प्रभावित थी, पर कभी भी एक एकङ से बङी नहीं हो सकती थी।
चौकी
सीमा-शुल्क चौकी।
कौङी
विनिमय के माध्यम की तरह प्रयुक्त सीपियां।
दरोगा
पुलिस, सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क का प्रमुख
दीवानी
किसी प्रांत का कर एकत्र करने का अधिकार
फरमान
शाही आदेश या फरमान
गंज
व्यापार केन्द्र अथवा बाजार
हासिल
किसी क्षेत्र से वास्तव में एकत्रित भूमि कर।
हाट
समय-समय पर लगने वाले ग्रामीण मेले।
इनाम
किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले प्राप्त कर मुक्त भूमि या अन्य उपहार।
इक्ता
दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारियों को उनके वेतन के बदले प्राप्त भूमि की इकाई जिसका कर उन्हें सौंपा जाता था।
जागीर
दिल्ली सल्तनत के इक्ता का मुगलकालीन समतुल्य।
जमा
किसी क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कुल अनुमानित भूमि कर।
जमाबंदी
किसी क्षेत्र, गांव अथवा जिले के आकलित कर का बंदोबस्त।
कारखाना
दिल्ली सल्तनत तथा मुगलकाल में शाही दरबार तथा सेना के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण करने वाला शआही कारखाना।
खालिसा
शाही अथवा राज्य की भूमि।
मदद-ए-माश
ऐसी भूमि जिसका कर राज्य द्वारा धार्मिक तथा विद्वान व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को सौंप दिया गया था।
मालिकाना
जमींदार के भूमि पर बेहतर अधिकारों के कारण राज्य द्वारा जमींदारों को भूमिकर का विशेष भत्ता।
मंडी
थोक बाजार।
मनौतीदार
बैंकर अथवा साहूकार जो एक राशि (मनौती) लेकर मध्यस्थ कर संग्रहकर्ता के लिये गारंटी प्रदान करता था।
मिल्की
भू स्वामित्व।
मोहर
स्वर्ण मुद्रा।
माउफी
कर मुक्त भूमि।
नजराना
निम्नतर व्यक्तियों द्वारा उच्चतर व्यक्तियों को दिया जाने वाला उपहार जो कि अकसर जबर्दस्ती लिया जाता था।
मुकर्ररी
निश्चित लगान अथवा दर पर भू-धारिता।
पट्टा
कर अधिकारियों द्वारा करदाताओं को दिया गया पत्र जिसमें दी जाने वाली रकम तथा भू-धारिता की शर्तों का विवरण होता था।
पट्टीदारी
किसी ग्राम अथवा क्षेत्र का संयुक्त स्वामित्व।
कबूलियत
वह पत्र जिसमें करदाता सरकार द्वारा नियत नियमों तथा शर्तों को स्वीकार करता था।
तक्कवी
उत्पादन के लिये सरकार द्वारा कृषकों को दी गयी अग्रिम राशि अथवा ऋण।
तिनकठिया
एक प्रणाली जिसके अंतर्गत यूरोपीय नीलरोपकों ने पूर्वी भारत में स्थानीय जमींदारों से ठीका पर भूमि लेकर अपनी भूमि पर कृषकों से, अत्यंत कम कीमत पर, नील बोना अनिवार्य कर दिया, तथा अगर वे नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते तो उन्हें शरहबेशी (बढा हुआ लगान) या तवान (मोटा-मोटी भुगतान) या कभी-कभी दोनों ही देना पङता था।
वतन
वंशानुगत भूमि
जेरात
यह प्रणाली जिसके अंतर्गत पूर्वी भारत में यूरोपीय नीलरोपकों ने ठीकेदारी पर भूमि लेकर उन पर अत्यंत कम भुगतान कर, कृषि मजदूरों की सहायता से नील उगाना प्रारंभ किया।
References : 1. पुस्तक- भारत का इतिहास, लेखक- के.कृष्ण रेड्डी