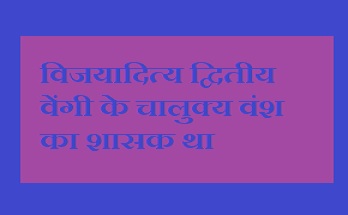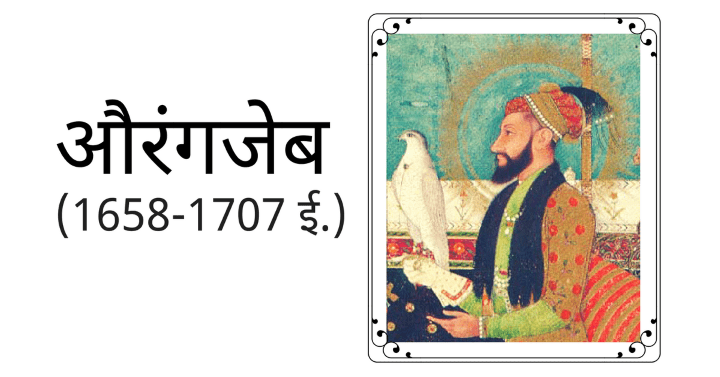मुगलों की भू राजस्व प्रणाली
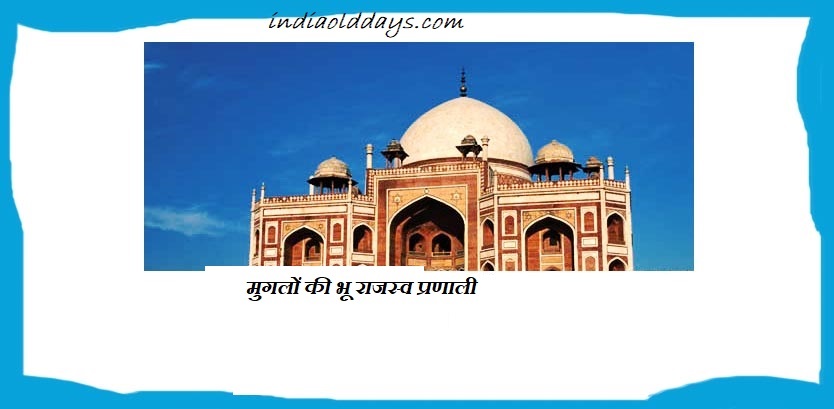
अन्य संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य-
- मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्थाः केन्द्रीय शासन
- दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय(इक्ता) व्यवस्था क्या थी
- मुगल काल की न्याय प्रणाली
- मुगलों की भू राजस्व प्रणाली
- मुगल भू-राजस्व अधिकारी
- मुगल काल में जागीरदारी प्रथा कैसी थी
- मुगलकालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी
- मुगल भू-राजस्व दर क्या थी
मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है
- केन्द्रीय आय के स्रोत एवं
- स्थानीय स्रोत।
भूमिकर के बँटवारे को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुगल भूमि को तीन भागों में बाँटा गया था-
- खालिसा भूमि शाही भूमि होती थी और इस भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी।
- जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के ऐवज में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूल करने का अधिकार होता था किन्तु प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था।
- सयूरगल या मदद-ए-माश भूमि को अनुदान के रूप में विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था।जिस पर अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था।यद्यपि यह भूमि अधिकतर अनुत्पादक होती थी।
प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनायी गयी जाब्ती प्रणाली को अपनाया जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था।
किन्तु जाब्ती (जाब्ती-ए-हरसाला) प्रणाली के अत्यंत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण 1568ई. में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नस्क अथवा कनकूत व्यवस्था को शुरू किया गया।
मुगलों के समय में प्रचलित विभिन्न भूराजस्व प्रणालियां निम्नलिखित थी-
-
जाब्ती-ए-दहसाला प्रणाली –
जाब्ती प्रणाली भूमि की पैमाइश एवं गल्ले की किस्म पर आधारित कर – प्रणाली थी यह प्रणाली बिहार,इलाहाबाद,मालवा,अवध,आगरा,दिल्ली,लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी।
गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू-राजस्व पर विशेष ध्यान दिया।फलस्वरूप उसने 1573ई. में बंगाल,बिहार और गुजरात को छोङकर समस्त उत्तर भारत में करोङी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनकी संख्या 182 थी।
करोङी का मुख्य कार्य- एक करोङ दाम (2,50,000 रु. क्योंकि 1रु.=40दाम) राजस्व के रूप में एकत्र करना था।
अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष (1580ई.) में आइने-दहसाला(टोडरमल बंदोबस्त) नामक एक नयी कर-प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया।
इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता -टोडरमल (ख्वाजाशाह मंसूर ने भी सहायता की थी) थे इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है।
इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी नकद रूप में करनी पङती थी। दहसाला प्रणाली में यद्यपि कर का निर्धारण पिछले दस वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था लेकिन उसका 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माल-ए-हरसाला कहा जाता था।
दहसाला प्रणाली हर संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की जाती थी।बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित हुई जिन क्षेत्रों में जाब्ती प्रणाली प्रचलित थी।
आइने दहसाला प्रणाली एक प्रकार की रैय्यतवाङी व्यवस्था थी क्योंकि इसमें सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे।
आइने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहाँ के शासन काल में मुर्शिद कुली खाँ ने लागू किया था।
इस बंदोबस्त के तहत खालिसा और जागीर दोनों प्रकार की भूमि को लिया गया था।
कालांतर में इस प्रणाली में और सुधार किया गया जिसके अंतर्गत हर सूबे में ऐसे परगने,जिनकी उर्वरता एक समान थी मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गयी।
-
भू राजस्व गल्ला बख्शी प्रणाली-
मुगलकाल में कर – निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली –बँटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे भाओली भी कहा जाता था।
इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इसमें भी उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था।
इस प्रणाली में राजस्व निर्धारण तीन तरह का होता था-
- खेत-बटाई- इसमें फसल तैयार होते ही खेत को बाँट लिया जाता था।
- लंक -बटाई – फसल कटने के बाद गट्ठर बांध कर उसे बाँट लिया जाता था।
- राशि – बटाई – अनाज तैयार होने के बाद बंटवारा होता था।
बंटाई प्रणाली सिंध,काबुल के कुछ भाग कंधार और कश्मीर में प्रचलित थी।
-
नस्क प्रणाली-
आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि नस्क अथवा कनकूत कर-निर्धारण की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी बल्कि कृषि-कर का लेखा-जोखा करने वाली प्रणाली थी।
कनकूत प्रणाली बटाई का संशोधित रूप था। इसे दाना बंदी भी कहा जाता था।
नस्क या कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का अंदाजा लगाकर (कच्चा अनुमान) जमीदारों या भू-स्वामियों से लगान की व्यवस्था की जाती थी यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी।
नस्क या कनकूत प्रणाली बंगाल,गुजरात और काठियावाङ क्षेत्रों में प्रचलित थी।
भू – राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण चार भागों में किया था। जो इस प्रकार है-
- पोलज – जिस पर हर वर्ष खेती होती हो।
- परती – जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोये छोङ दिया जाता था तो वह परती कहलाती थी।
- चाचर – जिसे तीन-चार वर्षों तक बिना बोये छोङा जाता था।
- बंजर – यह चार-पांच वर्षों तक या उससे अधिक समय तक बिना बोये पङी रहती थी।
काश्त कर खेती में प्रयुक्त भूमि पर ही लिया जाता था।
क्षेत्रफल की ईकाई बीघा मानी जाती थी।
अकबर ने सूर्य की गणना पर आधारित इलाही-संवत चलाया इसे फसली-संवत भी कहा जाता था।
अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए अपने शासन काल के 31वें वर्ष (1586-87 ई. ) में सिकंदरी गज(39इंच या 32इंच) के स्थान पर इलाहीगज (41इंगुल या 33 1/2इंच ) का प्रयोग आरंभ किया। जबकि इसके पूर्व भूमि की पैमाइश में सिकंदरी-गज का ही प्रयोग होता था।
किन्तु शाहजहाँ के काल में नाप में पुनः परिवर्तन हुआ। उसने दो नयी नापों को आरंभ किया-
- बीघा-ए-इलाही
- दिरा-ए-शाहजहाँनी(बीघा-ए-दफ्तरी)।
समकालीन इतिहासकार सादिक के अनुसार – मदद-ए-माश भूमि तो बीघा-ए-इलाही से नापी जाती थी परंतु सरकारी अभिलेखों के लिए भूमि दिरा-ए-शाहजहानी या बीघा – ए- दफ्तरी से नापी जाती थी।
औरंगजेब के पश्चात बीघा-ए-दफ्तरी का प्रयोग बंद हो गया किन्तु बीघा -ए-इलाही मुगल काल के अंत तक चलता रहा।
इसके अतिरिक्त अकबर ने तनब (तंबू की रस्सी) की जगह जरीब (बाँस का डंडा जिस पर लोहे की कङियाँ जुङी होती थी) का प्रचलन प्रारंभ किया । जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर पहला शासक था।
इस प्रकार दहसाला व्यवस्था न तो दस वर्षीय व्यवस्था थी और न ही स्थायी बंदोबस्त था। राज्य को इसमें संशोधन करने का अधिकार भी था।
कनकूत प्रथा में खेती को पगों तथा रस्सी से नापा जाता था,तत्पश्चात प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके राजस्व वसूल किया जाता था।
नस्क प्रथा कश्मीर में कनकूत प्रथा का एक विकल्प थी कश्मीर में इस प्रथा गल्ला-ए-बख्श तथा गुजरात में इसे नस्क-ए-जुज अथवा आंशिक नस्क कहा जाता था।
मुगलकालीन भूराजस्व के अन्य स्रोत-
मुगल काल में भू-राजस्व (खिराज ) के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक सामाजिक एवं स्थानीय कर लिये जाते थे।
बाबर और हुमायूँ ने हिन्दुओं से जजिया तथा मुसलमानों से जकात नामक कर वसूल किया।
भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात से ही यहाँ के हिन्दुओं से जजिया नामक कर वसूल किया जाने लगा था।
जजिया सामान्यतः ब्राह्मणों,साधु-संयासियों, अनाथों तथा स्रियों से नहीं लिया जाता था किन्तु फिरोजतुगलक के समय में यह इन लोगों से भी वसूव किया जाता था।
मुगल शासकों में बाबर तथा हुमायूँ ने भी हिन्दुओं से जजिया कर वसूल किया था। किन्तु 1664ई. में अकबर ने पहली बार इस धार्मिक कर को समाप्त कर दिया।
किन्तु औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के चलते इस कर को 1679 में पुनः लागू कर दिया किन्तु 1713ई. में फर्रुखसियर ने इसे पुनः समाप्त कर दिया।
जजिया का निर्धारण तीन श्रेणियों में किया गया था जो आय के आधार पर वसूल किया जाता था-
- 10हजार दिरहम से अधिक संपत्ति वालों से 48 दिरहम जजिया के रूप में वसूला जाता था।
- 200दिरहम से 10हजार दिरहम संपत्ति वाले व्यक्ति से 24 दिरहम वसूल किया जाता था।
- 200दिरहम से कम संपत्ति वाले व्यक्ति से 12दिरहम वसूल किया जाता था।
- मुगल प्रशासन से जजिया 1720 में मुहम्मद शाह के शासन काल में जाकर अंतिम रूप से समाप्त हुआ।
- जकात मुसलमानों से उनकी संपत्ति की राज्य द्वारा सुरक्षा करने के एवज में ढाई प्रतिशत (संपत्ति का 40वाँ भाग) की दर से वसूला जाता था।
- किन्तु मुगल सम्राटों द्वारा इस कर को केवल आयात या सीमा-शुल्क के रूप में ही लिया जाता था।
- अकबर ने अपने शासन काल में जिन करों को बंद किया था उनमें जकात भी एक कर था।किन्तु राजसी मनाही होने के बावजूद यह किसी न किसी रूप में लिया जाता रहा फलस्वरूप औरंगजेब को इस कर को न लेने की पुनः मनाही करनी पङी।
- खुम्स मूलतः युद्ध में लूट के माल का भाग होता था।, जिसके 1/5भाग पर राज्य का तथा 4/5भाग पर सैनिकों का हक होता था।
- मुगलकाल में खुम्स नामक कर समाप्त हो गया क्योंकि मुगल सैनिक वेतन भोगी होते थे।इस प्रकार युद्ध या लूट में प्राप्त संपूर्ण सम्पत्ति राज्य को प्राप्त होती थी।
- मुगल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं तथा मनसबदारों द्वारा समय-2 पर जो पेशकश(नकदी) या नजर प्राप्त होती थी उससे भी राज्य की आय में वृद्धि होती थी।
- 1700ई. में औरंगजेब ने आज्ञा दी कि नकद पेशकश को नजर कहा जाये तथा शाहजादों द्वारा सम्राट को दिये गये उपहार को नियाज एवं अमीरों के उपहार को निसार कहा जाए।
- मुगल काल में रिस वारिस विहीन अमीर की संपत्ति को राजगमिता कानून द्वारा बैतुलमाल (शाही खजाना) में जमा कर लिया जाता था।
- अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा चलाई। इसके लिए शुल्क लगता था।
- जहाँगीर ने अपने शासन काल में तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था।
Reference : https://www.indiaolddays.com/