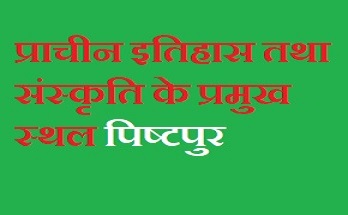राष्ट्रकूट शासकों का प्रशासन कैसा था
राष्ट्रकूट शासकों का राजत्व वस्तुतः अनुवांशिक था तथा सबसे बङा अथवा सबसे योग्य बेटा गद्दी पर आता था। युवराज अथवा उत्तराधिकारी का चुनाव राजा अपने जीवन में ही कर लेता था। युवराज आमतौर पर राजधानी में रहता था तथा राज के प्रशासनिक मामलों में मदद देता था और कभी-2 सैन्य अभियानों में भी राजा के साथ होता था। छोटे राजकुमारों को आमतौर पर प्रांतों का वजीर बनाया जाता था।
राष्ट्रकूट शासकों का इतिहास में योगदान।
राजा को राज्य का प्रशासन चलाने में मदद करने के लिये एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सेनापति एवं पुरोहित होते थे।
राष्ट्रकूट राज्य का कुछ भाग क्षत्रपों के अधीन था तथा कुछ भाग पर राज्य का सीधा प्रशासन था। महत्त्वपूर्ण सामंत लगभग पूर्णतः स्वतंत्र थे, पर उन्हें शाही दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था, उन्हें नियमित लगान देना होता था तथा एक निश्चित संख्या में सैनिक उपलब्ध कराने होते थे।
राष्ट्रकूट राज्य कई प्रांतों अथवा राष्ट्रों में विभाजित था, जो विषय अथवा जिलों में विभाजित थे। विषय पुनः भुक्तियों में विभाजित होते थे, जो 50 से 70 गांवों को मिलाकर बना होता था। भुक्ति 10 से 20 गांवों के छोटे समूहों में बंटा होता था।
क्षेत्रीय प्रशासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता था। उसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के उपर काफी अधिकार होता था। विषयपति अथवा जिलाधिकारी तथा भोगपति अथवा तहसील अधिकारी भी राष्ट्रपति के तरह की शक्तियों का अपने सीमित क्षेत्र में प्रयोग करते थे। कुछ विषयपतियों को क्षेत्रीय वजीर का स्तर प्राप्त था। भुक्ति का प्रधान भोगपति होता था तथा उसकी नियुक्ति सीधे केन्द्र सरकार के द्वारा की जाती थी। भोगपति नलगवंदों अथवा देशग्रामुक्तों की मदद से, जिनका पद आनुवांशिक होता था, राजस्व प्रशासन चलाते थे। गांवों के स्तर पर प्रशासन ग्राम प्रमुख तथा लेखापाल द्वारा चलाया जाता था, जिनका पद आमतौर पर आनुवांशिक होता था।
ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीण सभाओं अथवा समीतियों ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीण सभाओं अथवा समितियों ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण सभाएं अनेक उप-समितियों में विभाजित होती थी। हरेक उप-समिति एक खास काम के लिये उत्तरदायी होती थी, जैसी गांव का तालाब, मंदिर, सङक इत्यादि। राष्ट्रकूट स्रोतों में कहीं-2 विषय – महरात तथा राष्ट्र महारत का उल्लेख मिलात है, जिससे जिला प्रांतीय मुख्यालयों में इन लोकप्रिय परिषदों के होने का प्रमाण मिलता है।
साहित्य
इस काल में संस्कृत साहित्य को प्रश्रय प्रदान किया गया। राष्ट्रकूट दरबार में अनेक विद्वान थे। नालचंपु के रचयिता त्रिविकाराम 10 वी.शता. के उत्तरार्द्ध में हुए। हालयुद्ध ने कविरहस्य की रचना कृष्ण- III के शासन काल में की।
राष्ट्रकूटों द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने पर जैन साहित्य ने स्वाभाविक रूप से दौरान काफी विकास किया। अकलंक तथा विद्यानंद ने अष्टसती तथा अस्टसस्त्री की रचना की, जो कि आप्तमीमांसा पर टिप्पणियां हैं। तर्क के क्षेत्र में मानिक्यनंदिन ने परीक्षामुखसहस्र की रचना 8 वी. शता. के पूर्वार्द्ध में की। उन्होंने न्यायकौमुदीचंद्रोदय के नाम से एक स्वतंत्र रचना की। अमोघवर्ष-I के धार्मिक गुरु हरिसेन ने हरिवंश की रचना की। वे आदिपुराण पूरा नहीं कर पाए, जो विभिन्न जैन संतों की जीवनी है। इसे उनके शिष्य गुनाभद्र ने पूरा किया। जिनसेन की पारस्वम्युदय परस्व की जीवनी है, जो कि छंद शैली में लिखी गई है। अमोघवर्ष के शासनकाल में ही व्याकरण पर शाकातयान द्वारा रचित अमोघवृद्धि तथा गणित पर वीरचर्या की गणितसरसम्ग्रहक की रचना की गई।
राष्ट्रकूट काल में ही कैनरी साहित्य प्रारंभ हुआ। कैनरी काव्यशास्र पर पहली पुस्तक कविराजमार्ग के रचयिता खुद अमोघवर्ष -l थे। कैनरी काव्य के प्राचीनतम तथा महानतम रचनाकार तथा आदिपुराण और विक्रमराजुनाविजया के लेखक पंपा-l 10 वी. शता. के उतरार्द्ध में हुये। शांतिपुराण के लेखक पोन्ना 10 वी. शता. के तीसरे भाग में हुए वे भी एक प्रख्यात कवि थे।
References : 1. पुस्तक- भारत का इतिहास, लेखक- के.कृष्ण रेड्डी