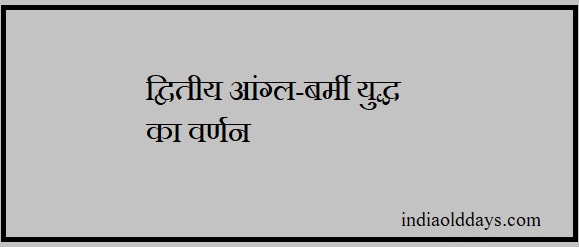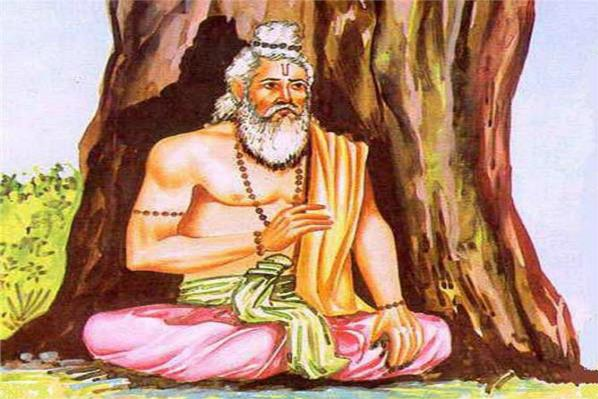डरबन का पृथ्वी सम्मेलन क्या था
डरबन का पृथ्वी सम्मेलन (Durban’s Earth Conference)
डरबन का पृथ्वी सम्मेलन – 8 सितंबर, 2003 को दक्षिण अफ्रीका में डरबन में संसार के पर्यावरणविदों का 10 दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां संसार के विभिन्न देशों के 2500 के लगभग संरक्षण विशेषज्ञ एकत्र हुए। यहां संसार के संरक्षित क्षेत्रों तथा विविधता की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया। यहां स्पष्ट किया गया कि संसार के संबसे कम विकसित देश पृथ्वी के खतरे से झूझ रहे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिये साधन जुटाने में असमर्थ हैं तथा विश्व के समृद्ध देशों को इसकी आर्थिक जिम्मेदारी लेनी चाहिये।
यहां यह बात सामने आई कि धरती का 11.5% संरक्षित क्षेत्र है किन्तु अधिकांश, विशेषकर समुद्री पर्यावरणीय तंत्र के संरक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। विश्व की 10% से कम बङी झीलों की संरक्षण व्यवस्था की गई है तथा समुद्र का 5% से भी कम क्षेत्र में आता है। दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र वर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के 10 वें सम्मेलन में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि पर गंभीर चिंतन हुआ।
किन्तु अभी भी जिनके मन में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता व इसके संबंध में गहरी संवेदना है ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन एक जन आंदोलन बन जाना चाहिये, क्योंकि हम सभी का तथा आने वाली पीढियों का पृथ्वी पर निर्वहन इससे जुङा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने तथा घटते हुए संसाधनों के संरक्षण के लिये और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्र की लहरों से ऊर्जा तथा गोबर गैस प्लांट आदि की जानकारी का विस्तार हो रहा है।
आबादी की वृद्धि रोकनी होगी यह एक सामान्य जानकारी की बात है। शहरों की सीवरेज और उद्योगों के प्रदूषित जल को प्रदूषण रहित करके नदियों या तालाबों में छोङा जाना चाहिए यह सब जानते हैं। भू जल के स्तर के घटने की बात भी सभी जानने लगे हैं। मृदा के कटाव और रासायनिक खादों तथा कीट नाशकों से होनो वाली हानि की किसानों को जानकारी हो रही है। वायु के प्रदूषण के कारण नगरों में बच्चों को मास्क लगाकर सङकों पर निकलना पङ रहा है। वनों की कटाई से होने वाले नुकसान की जानकारी सामान्य लोगों को भी होने लगी है। इन सब पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी के साथ ही इनके निदान के उपाय करने की प्रतिबद्धता उत्पन्न होनी चाहिये।
तकनीकी जानकारी और विज्ञान के विकास ने सभी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। किन्तु इसका उपाय विज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। जो विनाश हुआ है उसकी जिम्मेदारी विज्ञान की नहीं अपितु हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण की है। मनुष्य ने मूर्खतावश ऐसी संस्कृति विकसित की है जिसमें भोगवाद, उपभोक्तावाद तथा दिखावे को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है।
आज टेलीविजन और अखबारों के प्रचार तंत्र पर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है जिनका काम अपने उत्पादों को बेचना है। ये उत्पाद अधिकांशतया जीवन की मूल आवश्यकताओं से संबंध नहीं रखते। इनमें से अधिकांश का संबंध अनावश्यक सुख सुविधायें जुटाने, भोगवाद और दिखावे-प्रदर्शन से होता है। विकसित और विकासशील देशों के धनिकों के जीवन को देखकर सामान्य लोगों के मन में उनकी जीवन पद्धति का अनुकरण करने की प्रवृत्ति के साधनों का उपभोग करने लगे तो धरती के लिये कुछ समय के लिये भी इसको सहन कर पाना संभव नहीं होगा। इससे सारा पर्यावरण तंत्र छिन्न-भिन्न हो जायेगा।
यह धरती हमारी साझी विरासत है। इसमें सुखी संपन्न और तनाव युक्त जीवन यापन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस धरती के पर्यावरण की रक्षा संसार के सभी विकसित और विकासशील तथा अमीर और गरीब लोगों का कर्त्तव्य है। इस दृष्टि से विकसित देशों और धनी लोगों का दायित्व अधिक बढ जाता है। उनके जीवन में संयम और अपरिग्रह आवश्यक है। उनके आत्म नियंत्रण से संसार के गरीब देशों और गरीब लोगों की वृथा आकांक्षाओं में कमी होगी जो प्रतियोगिता और तनाव का कारण होती है।
यदि संसार के साधनों का बुद्धि पूर्वक उपयोग होने लगे तथा हथियारों और विलास की सामग्री का उत्पादन बंद हो सके तो धरती माता सबकी आवश्यकता को पूरी करने में सक्षम है तथा मनुष्य की लोभ की प्रवृत्ति और मूर्खता से धरती पर हुए घाव भी भर सकते हैं। अथर्ववेद में धरती को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहा गया है। धरती के पुत्रों को इसे माता मानकर व्यवहार करना होगा तभी धरती का प्रकोप शांत होगा।