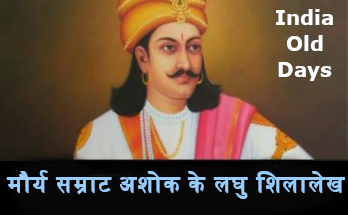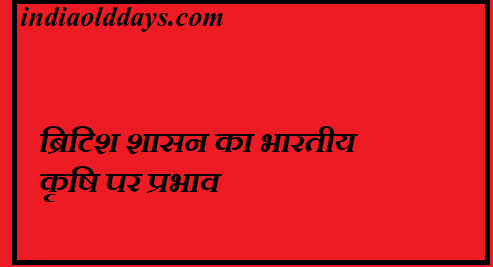भारत सरकार अधिनियम,1919 का इतिहास (Government of India Act, 1919)
किसी भी देश के संविधान को भलीभाँति समझने के लिए उसके विकास का इतिहास जानना आवश्यक होता है। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासन के इतिहास से जुङा हुआ है।
1857 ई. की क्रांति की समाप्ति के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम, 1858 पारित किया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया तथा भारतीयों के ह्रदय को पुनः जीतने के लिए महारानी विक्टोरिया की घोषणा प्रसारित की गयी, जिसमें भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि अब भारत का प्रशासन प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए चलाया जायेगा। किन्तु वास्तव में प्रशासन की दुकान वही रही, केवल दुकान का बोर्ड बदल दिया गया।
फलस्वरूप भारतीयों में असंतोष उत्पन्न होने लगा और भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। इसलिए 1858 ई. से 1947 ई. तक के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष का परिणाम था। इसलिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास एक दूसरे से इतने जुङे हुए हैं कि एक का अध्ययन दूसरे के बिना संभव नहीं है।
1919 के पूर्व भारत में संवैधानिक विकास
सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद ने 1858 ई. में एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया तथा ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिये गये। इनके स्थान पर भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया कौंसिल बनायी गयी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर-जनरल के पदनाम से तथा देशी राज्यों से संबंध स्थापित करते समय उसे वायसराय के पदनाम से पुकारने की व्यवस्था की गई।
भारत के गवर्नर,गवर्नर जनरल एवं वायसराय
इस अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गयी। किन्तु इस अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में परिवर्तन किया गया था, अतः भारत के प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन करना अनिवार्य था। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 6 जून, 1861 को भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया।
इस अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या पाँच कर दी गयी। यह भी व्यवस्था की गयी कि जब गवर्नर जनरल की कौंसिल किसी विधेयक को पारित करने हेतु बैठती थी, उस समय कुछ अतिरिक्त सदस्य भी उस बैठक में सम्मिलित होंगे। ऐसी बैठक जिसमें अतिरिक्त सदस्यों को बिल पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया हो, विधान परिषद कहते हैं। गवर्नर-जनरल अपनी विधान परिषद में कम से कम छः तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य मनोनीत कर सकता था, जिसमें आधे सदस्य गैर-सरकारी होंगे और उनका कार्यकाल दो वर्ष रखा गया। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से लेनी पङती थी।
बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को भी अपनी कौंसिल में कानून बनाने के लिए कम से कम चार और अधिक से अधिक 8 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। वस्तुतः इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना नहीं था, बल्कि गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल की निरंकुशता को बढाना था। विधान परिषदें कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकती थी।
1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने 1861 ई. के सुधारों को अपर्याप्त बताया है और विधान परिषदों के विस्तार तथा अधिक निर्वाचित सदस्यों की मांग की। अतः लार्ड डफरिन ने एक समिति नियुक्त की जिसने विधान परिषद को छोटी संसद के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1892 ई. में एक दूसरा भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार विधान परिषद के अलावा सदस्यों की संख्या बढा दी गयी।
अब कम से कम दस तथा अधिक से अधिक 16 सदस्य मनोनीत किये जा सकते थे। मद्रास तथा बंबई की विधान परिषदों में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 सदस्य मनोनीत किये जा सकते थे। अतिरिक्त सदस्यों में 2/5 सदस्य गैर-सरकारी होंगे। अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की ऐसी प्रणाली अपनाई गयी जो निर्वाचित और मनोनीत के मध्य की प्रणाली थी।
विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने तथा प्रश्न के उत्तर पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किन्तु पूरक प्रश्न पूछने तथा प्रश्न के उत्तर पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किन्तु पूरक प्रश्न पूछने तथा प्रश्न के उत्तर पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया। विधान परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना कारण बताये किसी प्रश्न के पूछने की अनुमति अस्वीकृत कर सकता था।
इस अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि कार्यकारिणी अपनी नीतियों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी की निरंकुशता ज्यों की त्यों बनी रही।
1892 ई. से 1909 ई. के मध्य का समय तूफान और दबाव का समय था। लार्ड कर्जन ने 1905 ई. में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसने देश में बढते हुए असंतोष में आहुति का कार्य किया। बंग-भंग आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया, जिसको सरकार ने अपनी पूर्ण शक्ति से कुचल दिया। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय काँग्रेस में फूट पङ गयी और उदार तथा उग्र विचारधारा वाले दो दल बन गये। इस फूट का लाभ उठाकर सरकार ने उदारवादियों की पीठ थपथपाने के प्रयत्न आरंभ कर दिये।
गवर्नर जनरल लार्ड मिण्टो राष्ट्रवाद के वेग को रोकने के लिए हिन्दू-मुसलमानों में फूट पैदा करने के प्रयत्न आरंभ कर दिये। उसने मुसलमानों को विधान परिषद में अलग प्रतिनिधित्व देने की माँग करने हेतु प्रोत्साहित किया। गवर्नर जनरल से प्रोत्साहित होकर मुसलमानों ने अपने लिए विधान परिषदों में अलग प्रतिनिधित्व की माँग की और 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। लार्ड मिण्टो ने सुधारों की एक योजना भारत सचिव मॉर्ले के पास भेजी।
यह योजना एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गयी। ब्रिटिश संसद ने इसे 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से पारित कर दिया । इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 69 निश्चित की गयी, जिनमें 9 पदेन (कार्यकारिणी के सदस्य) तथा 60 अतिरिक्त सदस्य रखे गये।
अतिरिक्त सदस्यों में 28 सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 निर्वाचित तथा 5 मनोनीत होंगे। 27 निर्वाचित सदस्यों में से 5 मुसलमानों द्वारा, 6 हिन्दू जमींदारों द्वारा, एक-एक मुस्लिम जमींदारों, बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स तथा बंबई चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुने जायेंगे। शेष 13 सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जायेंगे। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया।
बंबई, मद्रास बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 50 कर दी गयी। छोटे प्रांतों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 30 कर दी गयी। विधान परिषदों के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गयी। अब उस सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया जिसने मूल प्रश्न किया हो। बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया, किन्तु बजट के कुछ विशेष मदों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था और न बजट पर मतदान करवाया जाता था।
विधान परिषद का अध्यक्ष सार्वजनिक हित का बहाना लेकर किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अस्वीकृत कर सकता था। यह अधिनियम निश्चित रूप से 1892 के अधिनियम से अच्छा था। किन्तु इससे कार्यकारिणी और विधान परिषद के संबंधों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पङा, क्योंकि कार्यकारिणी पूर्व की भाँति स्वेच्छाचारी बनी रही। इस अधिनियम ने भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के विशेष तत्वों का ऐसा बीजारोपण किया जो 1947 ई. में देश-विभाजन के रूप में पल्लवित हुआ।
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
1909 ई. के सुधारों से भारतीयों की क्षुधा शांत नहीं हो सकी। भारत में राजनैतिक असंतोष दिन-प्रतिदिन बढता गया, जिसके फलस्वरूप देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी क्रियायें बढ गई।
1910 ई. में भारतीय प्रेस एक्ट(Indian press act) पारित करके समाचार -पत्रों की स्वतंत्रता को कुचल दिया। 1911 ई. में राजद्रोह सभा अधिनियम पास करके सरकार ने सभाएँ करने पर रोक लगा दी…अधिक जानकारी