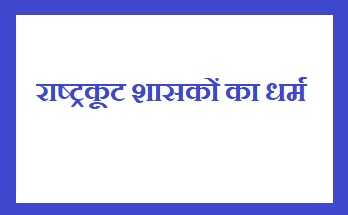वेद के दो भाग हैं – कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकाण्डों का विशिष्ट विवरण मिलता है तथा उपनिषद् में ज्ञानकांड का प्रतिपादन है। मीमांसा, जिसे पूर्व-मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्मकाण्डों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है। यह मत वेद को अपौरुषेय तथा नित्य मानता है। अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न इस दर्शन में मिलता है। उपनिषद् तथा वेदांत उत्तरमीमांसा कहे जाते हैं,क्योंकि इनमें कर्मकाण्डों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है।
पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनि है, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। शबर स्वामी ने इस पर विस्तृत टीका लिखी है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं, जिनके नाम पर मीमांसा के दो स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल हैं।
मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत
प्रमाण
मीमांसा दर्शन छः प्रमाणों को स्वीकार करता है – प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अंतिम प्रमाण को केवल भाट्टमीमांसक स्वीकार करते हैं।
मीमांसा दर्शन दो प्रकार के ज्ञान मानता है – प्रत्यक्ष तथा परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान केवल सत् पदार्थों का ही हो सकता है। किसी ज्ञानेन्द्रिय के साथ सत् (वर्तमान)विषय या पदार्थ का संपर्क होने पर ही उस विषय का प्रत्यक्ष या यथार्थ ज्ञान आत्मा हो सकता है। कुमारिल ने साक्षात् प्रतीति को प्रत्यक्ष बताया है – साक्षात प्रतीतिः प्रत्यक्षः। इस प्रकार का ज्ञान वस्तुतः समस्त दोषों से मुक्त होता है। मीमांसा के प्रत्यक्ष विषय का विचार सामान्यतः न्याय दर्शन के ही समान है। मीमांसकों का अनुमान संबंधी विचार भी नैयायिकों जैसा ही है।
उपमान
मीमांसक भी नैयायिकों के समान उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, किन्तु उनका मत कुछ भिन्न प्रकार का है।न्याय मत में संज्ञा संज्ञि (नामनामी) संबंध के ज्ञान को उपमान कहा जाता है।जैसे यदि कोई विश्वनीय व्यक्ति हमारे सामने किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करता है, जिसे हमने कभी नहीं देखा है तथा हम उस वर्णन के आधार पर भविष्य में यदि उसी प्रकार की वस्तु को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमारा यह ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त होता होगा।
किन्तु मीमांसा के अनुसार जब हम पहले देखी गयी वस्तु के समान बाद में दूसरी वस्तु देखकर जान लेते हैं, कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान है, तभी उपमान प्रमाण होता है। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति ने गाय देखी है, किन्तु नील गाय नहीं देखी है। बाद में नील गाय देखकर अपने पूर्वज्ञान के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है,कि गाय नीलगाय के समान होती है तो यह ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त कहा जायेगा। इस प्रकार जहाँ न्याय में उपमान के लिये पहले वस्तु का प्रत्यक्ष वर्णन आवश्यक नहीं है वहाँ मीमांसा प्रत्यक्ष दर्शन को आवश्यक मानती है। यहाँ किसी आप्त वचन की आवश्यकता नहीं है, अपितु स्वतः स्मृति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
शब्द
मीमांसा में शब्द प्रमाण का सर्वाधिक महत्त्व है। विश्वसनीय व्यक्तियों के वचन (आप्तवाक्य) तथा वेदों का विवरण शब्द प्रमाण है। आप्तवाक्य को पौरुषेय तथा वेदवाक्य को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद को यहाँ स्वतः प्रमाण माना गया है, जो नित्य तथा समस्त ज्ञान का आधार है। ऋषि वैदिक मंत्रो के रचयिता न होकर द्रष्टामात्र हैं।
प्रभाकर केवल वेद वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं तथा आप्तवाक्य को अनुमान की कोटि में रखते हैं। वेदवाक्य दो प्रकार के माने गये हैं – सिद्धार्थ अर्थात् जिससे किसी सिद्ध विषय का ज्ञान हो तथा विधायक अर्थात् वे वाक्य जो किसी क्रिया के लिये आज्ञापित करते हैं। इसी में यज्ञीय विधिविधानों का निर्देश रहता है। मीमांसक इसी को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। सिद्धार्थ वाक्य तभी तक मान्य है जब तक कि वह विधायक वाक्य का समर्थन करे।
अर्थापति
ज्ञान अर्थ की व्याख्या के लिये अज्ञात अर्थ की कल्पना अर्थात् जिसकी सहायता के बिना ज्ञात अर्थ को उपपत्ति न हो सके, को अर्थापत्ति कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जीवित है और वह अपने घर में नहीं है,तो अर्थापत्ति द्वारा हम यह ज्ञात कर लेते हैं, कि वह कहीं बाहर है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करता तथापि स्वस्थ्य है तो यह ज्ञात होगा कि वह रात में भोजन करता होगा। मीमांसक इस प्रकार के ज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं।
अनुपलब्धि
उपलब्धि (प्राप्ति) के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। इस प्रमाण को केवल कुमारिल तथा उनके अनुयायी स्वीकार करते हैं, प्रभाकर तथा उनके अनुयायी इसे नहीं मानते। इसके द्वारा हम किसी विषय के न होने (अभाव) का सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कमरे में घङा नहीं है यह ज्ञान हमें वहाँ घङे की अनुपलब्धि से ही हुआ। यह ज्ञान हमें किसी अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता। किन्तु केवल किसी वस्तु के न होने से अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होता।
घने अंधकार में घङा होने पर भी हम उसे नहीं देख पाते। पाप, पुण्य, परमाणु, आकाश आदि भी दिखाई नहीं देते किन्तु हम इसे अभाव नहीं मान सकते। अभाव का अर्थ यह है, कि जिस परिस्थिति में जो वस्तु होनी चाहिये उसका न होना। इसे योग्यानुपलब्धि कहा जाता है। वेदान्ती भी इसका समर्थन करते हैं।
प्रभाकर भट्ट तथा उसके अनुयायी अभाव का बोध कराने के लिये किसी स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं मानते। उनके अनुसार केवल पाँच प्रमाणों से ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं।
स्वतः प्रमाण्यवाद
मीमांसा दर्शन के अनुसार दोषरहित कारण सामग्री के पर्याप्त होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह यथार्थ ज्ञान है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखकर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का ज्ञान यथार्थ है और इसे पुष्ट करने के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। अतः मीमांसा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि ज्ञान की प्रामाणिकता उस ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहती हैं। उत्पादक सामग्री में दोष या त्रुटि होने पर ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता, जैसे पाण्डु रोगी को कभी भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। मीमांसकों का यह मत स्वतः प्रमाण्यवाद कहा जाता है। इसके अंदर दो बातें होती हैं –
ज्ञान की प्रामाणिकता उसकी उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहती है।
प्रामाणिकता का ज्ञान हमें उस ज्ञान के उत्पन्न होते ही हो जाता है। किसी दूसरे स्त्रोत से हमें उसकी परीक्षा नहीं करनी पङती।
यथार्थता अथवा विश्वसनीयता ज्ञान का स्वभाव ही है। यदि ज्ञान की उत्पादकता सामग्री में कोई दोष होता है, तो उससे उत्पन्न ज्ञान को हम यथार्थ नहीं कह सकते। मीमांसक नैयायिकों के इस मत को नहीं मानते हैं, कि ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये अन्य युक्तियों का सहारा लेना पङता है। नैयायिक मत परतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है।
मीमांसक ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानने के साथ स्वप्रकाश भी मानते हैं। उनके अनुसार नित्य नित्य एवं अपौरुषेय वेद भी स्वतः प्रमाण ही हैं, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये अन्य किसी उपादान की आवश्यकता नहीं पङती। मीमांसक वेद की प्रामाणिकता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुये उनका स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करते हैं।
मीमांसा दर्शन में भ्रम का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। प्रभाकर के अनुसार सभी ज्ञान सत्य होते हैं। जिसे हम भ्रम समझते हैं, उसमें भी दो प्रकार के ज्ञानों का योग रहता है। जैसे रस्सी में सर्प का जब आभास होता है, तो हमें एक टेढी-मेढी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा पहले देखे गये सर्प की स्मृति, ये दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं।
यहाँ ये दोनों ही बातें ही सत्य हैं। दोष केवल हमारी स्मृति का है। हमें प्रत्यक्ष तथा स्मृति के भेद का पता नहीं चल पाता, जिससे हम सर्प का व्यवहार रस्सी के साथ कर बैठते हैं। स्मृति के लोप के कारण हमें दोनों में भेद का पता नहीं लग पाता है। इस मत को अख्यातिवाद कहा जाता है, जो भ्रम की सत्ता का निषेध करता है।
कुमारिल तथा उनके अनुयायी उपर्युक्त मत को नहीं मानते। उनका कहना है, कि कभी-कभी मिथ्या वस्तु में सत्य की प्रतीति होने लगती है। जब हम रस्सी साँप है, ऐसा मान लेते हैं, तो दोनों की ही सत्ता है। भ्रम केवल यह है, कि हम दो अलग-अलग पदार्थों में उद्देश्य-विधेय का संबंध स्थापित कर देते हैं। विषय तो सत्य होते हैं, केवल संसर्ग का ही भ्रम पैदा हो जाता है। यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में गलत समझने का है, जो ज्ञान के कारणों में कुछ दोष के कारण उत्पन्न होता है तथा कालांतर में दूर हो जाता है।
किन्तु जब तक भ्रम की प्रतीति होती रहती है, यह अपने में ज्ञान के रूप में वैद्य रहता है। यह मत विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है, जिसमें कार्यता की प्रतीति अकार्य में हो जाती है अर्थात् जिस प्रकार के रूप में ज्ञान होना चाहिये था वह किसी दोष के कारण नहीं हो पाता, अपितु वह दूसरे प्रकार के रूप में होता है। इस विपरीत ज्ञान के कारण ही भ्रम को विपरीत ख्याति की संज्ञा दी जाती है।
किन्तु दोनों ही संप्रदाय इस मत से सहमत हैं, कि भ्रम का प्रभाव ज्ञान की अपेक्षा हमारे व्यवहार पर अधिक पङता है। दोनों भ्रम को अपवाद रूप में ग्रहण करते हैं। उनका कहना है, कि जगत का सामान्य नियम यही है, कि प्रत्येक ज्ञान सत्य तथा यथार्थ होता है। इसी मान्यता के आधार पर मनुष्य दैनिक जीवन में अपना व्यवहार चलाता है। लेकिन कभी-कभी इसमें जो अपवाद मिलता है, वही भ्रम है।
जगत् तथा उसके विषय
मीमांसा जगत् तथा उसके समस्त विषयों की सत्यता को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष विषयों के अलावा स्वर्ग, नरक, आत्मा तथा वैदिक यज्ञ के देवताओं के अस्तित्व को भी प्रमाणों के आधार पर इस मत में स्वीकार किया गया है। कर्म के सिद्धांत में इसका विश्वास है। कर्म के अनुसार ही सृष्टि की रचना होती है।
मीमांसा संसार की सृष्टि तथा उसके प्रलय को नहीं मानता।उसके अनुसार संसार की न तो कभी उत्पत्ति हुई है और न ही विनाश। केवल इसके मनुष्य तथा पदार्थों की उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है। जगत् की सत्ता निरंतर विद्यमान रहती है। कुछ मीमांसक वैशेषिक परमाणुवाद को भी मानते हैं, किन्तु उनके अनुसार परमाणुओं का परिचालक ईश्वर नहीं है। यह कर्म का सिद्धांत है, जो उन्हें प्रवर्तित करता है तथा जीवात्माओं को कर्मफल का भोग कराने के लिये संसार की रचना होती है।
इस प्रकार मीमांसा दर्शन अनेकवादी तथा वस्तुवादी है। इस लोक में हम यज्ञादि जो कर्म करते हैं उनसे एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे यहाँ अपूर्व कहा गया है। यह कर्म फल प्राप्त कराने वाली शक्ति है, जो आत्मा में निवास करती है। यह भविष्य में व्यक्ति को उसके कृत कर्म का फल प्रदान करती है। हम जो इस लोक में कर्म करते हैं, उसका फल हमें परलोक में प्राप्त हो सकता है। जगत् संचालन अपूर्व से ही होता है।
आत्मा, बंधन तथा मोक्ष
मीमांसा दर्शन अनेकात्मवाद का समर्थक है। इसके अनुसार जितने जीव हैं, उतनी ही आत्मायें हैं। ये नित्य, सर्वगत, विभु तथा व्यापक द्रव्य हैं, जो चैतन्य का आश्रय हैं। आत्मा को ज्ञाता, भोक्ता तथा कर्ता माना गया है। शरीर उसका भोगायतन है, बाह्य वस्तुएँ भोग्य पदार्थ हैं, तथा इन्द्रियाँ भोग कराने की साधन हैं। चैतन्य को यहाँ आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना गया है, अपितु यह एक आगन्तुक गुण है, जो मन तथा इन्द्रियों के संयोग से उसमें उत्पन्न हो जाता है।
जीवात्मा ही बंधनग्रस्त होता है तथा उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। बंधन तथा मोक्ष संबंधी मीमांसकों के विचार न्याय-वैशेषिक जैसे ही हैं। आत्मा का शरीर, इन्द्रियों तथा बाह्य पदार्थों से छुटकारा ही मोक्ष है। मीमांसा वेदान्त के इस विचार को नहीं मानता कि मोक्ष में आत्मा भौतिक जगत् से परे हो जाता है। सांख्य-योग के समान यह जगत् तथा आत्मा के संबंध को मिथ्या नहीं समझता। इनके विपरीत मीमांसा के अनुसार संसार नित्य है तथा आत्मा के मुक्त हो जाने पर भी उसी रूप में बना रहता है। मोक्ष की अवस्था में मात्र यह ज्ञान हो जाता है, कि आत्मा समस्त गुणों, सुख, दुःख, आनंद, चैतन्य आदि से विहीन होकर शुद्ध द्रव्य के रूप में रह जाता है। किन्तु बाद में कुछ भाट्ट मीमांसक मोक्ष की अवस्था को आनंदमय मानने लगे।
धर्म
मीमांसा दर्शन में धर्म का बहुत अधिक महत्त्व है। जैमिनि के अनुसार धर्म वह आदेश है, जो मनुष्य को कर्म के लिये प्रेरित करता है। धर्म का ज्ञान केवल अपौरुषेय वेदों से ही होता है। वेद जिसका विधान करते हैं, वह धर्म है तथा जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म है। वेदोक्त नियमों के अनुसार आचरण करने पर ही हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं।
मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्मकाण्डों पर अत्यधिक बल देते हुये प्रत्येक व्यक्ति के लिये उन्हें अनिवार्य रूप से करणीय बताया गया है। वेद-विहित यज्ञों तथा उनके कर्मकाण्डों का ठीक-ठीक अनुष्ठान करने का उपदेश मीमांसक देते हैं। कर्म तीन प्रकार के बताये गये हैं – अनिवार्य, ऐच्छिक तथा निषिद्ध। अनिवार्य कर्म दो प्रकार के हैं – नित्य अर्थात् प्रतिदिन किये जाने वाले (जैसे – पूजा, प्रार्थना आदि) तथा नैमित्तिक अर्थात् विशेष अवसरों पर किये जाने वाले।
ऐच्छिक कार्यों को काम्य कहा जाता है, जिनके करने से पुण्य प्राप्त होते हैं। निषिद्ध कर्मों को करने से पाप होता है। प्रारंभिक मीमांसक धर्म में ही विश्वास करते थे तथा उनका आदर्श स्वर्ग की प्राप्ति करना था। किन्तु बाद में मीमांसकों ने स्वर्ग के स्थान पर अपवर्ग (मोक्ष) को मान्यता दी। किन्तु यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिये ज्ञान के स्थान पर वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को ही साधन स्वीकार किया गया है। ज्ञान उस कर्म का सहायक होता है।
मीमांसा दर्शन कर्म को ही महत्त्व देता है, जो अपनी शक्ति (अपूर्व) से फल प्रदान करने में सक्षम है। इसके लिये वे ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं मानते। मीमांसकों के ईश्वर संबंधी विचार स्पष्ट नहीं है। इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है।
References : 1. पुस्तक- प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, लेखक- के.सी.श्रीवास्तव
India Old Days : Search