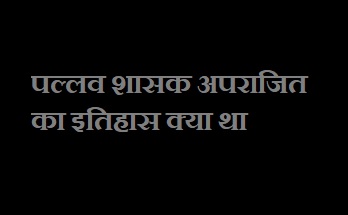प्राचीन काल में शिक्षण शुल्क
प्राचीन भारतीय शिक्षा में शुल्क प्रदान करने का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रायः शिक्षा निःशुल्क होती थी। शिक्षा प्रदान करना विद्वानों एवं आचार्यों का पुनीत कर्तव्य माना गया था। जो लोग शुल्क पाने की लालसा से शिक्षा प्रदान करते थे, समाज उन्हें निन्दा की दृष्टि से देखता था। कालिदास ने ऐसे विद्वानों को ज्ञान का व्यवसायी कहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था, कि निर्धन बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जायँ। तथापि शिष्य का यह कर्त्तव्य था, कि वह ज्ञानदाता आचार्य को कुछ न कुछ धन दक्षिणा के रूप में अवश्य प्रदान करें। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गयी ताकि आचार्य के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न न हो सके। धनी व्यक्ति अपने बालकों के प्रवेश के समय ही गुरु को संपूर्ण धनराशि प्रदान कर देते थे। जातक कथाओं से पता चलता है, कि श्रेष्ठिपुत्र तथा राजकुमार तक्षशिला में शिक्षा के लिये प्रवेश के समय ही संपूर्ण शिक्षण शुल्क दे देते थे। महाभारत से पता चलता है, कि भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव राजकुमारों की शिक्षा के निमित्त प्रारंभ में ही शुल्क प्रदान कर दिया था। यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुये भी आचार्य को शुल्क प्रदान नहीं करता था, तो समाज में उसकी निन्दा की जाती थी। जिन छात्रों के अभिभावक निर्धन होते थे, वे स्वयं गुरु की सेवा द्वारा शुल्क की क्षतिपूर्ति करते थे। अध्ययन समाप्ति के बाद ऐसे विद्यार्थी भिक्षा मांग कर गुरु-दक्षिणा चुकाते थे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहाँ आचार्यों ने दक्षिणा लेने से इन्कार कर कर दिया। याज्ञवल्क्य ने जनक द्वारा प्रदत्त दक्षिणा ग्रहण नहीं की।
बौद्ध-भिक्षु नागसेन ने मेनाण्डर द्वारा दी गयी दक्षिणा नहीं ली थी। कभी-कभी गुरु, शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर उसे ही दक्षिणा मान लेता था तथा शिष्य के हठ करने पर क्रुद्ध हो जाता था। रघुवंश से पता चलता है, कि वरतन्तु के शिष्य कौत्स ने जब गुरु-दक्षिणा देना चाहा तो गुरु ने उसकी सेवा को ही पर्याप्त माना,किन्तु बारम्बार हठ करने पर वे चिढ गये तथा दंड स्वरूप चौदह करोङ स्वर्ण मुद्रायें प्रदान करने को कहा। रघु की सहायता से कौत्स इतनी बढी धनराशि वरतन्तु को प्रदान करने में सफल रहा।
राज्य तथा समाज का कर्तव्य यह था, कि वह अध्ययन-अध्यापन करने वाले विद्वानों के निर्वाह की उचित व्यवस्था करे। इस उद्देश्य से शासक तथा कुलीन लोग शिक्षण संस्थाओं को भूमि तथा धनादि का दान देते थे।
गुप्त काल में ब्राह्मण विद्वानों को ग्राम दान में दिये जाते थे, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। चीनी स्त्रोतों से पता चलता है, कि हर्ष ने उङीसा में जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 14 बङे गाँव दान में दिये थे। नालंदा महाविहार को भी आस-पास के ग्राम दान में दिये गये थे। इन गाँवों से जो राजस्व मिलता था, उससे शिक्षण संस्थाओं का खर्च चलता तथा विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन, वस्त्र, आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती थी। गौतम तथा विष्णु जैसे शास्त्रकारों ने व्यवस्था दी है, कि छात्रों को निःशुल्क पढाने वाले आचार्य के भरण-पोषण की व्यवस्था राजा को करनी चाहिये। उसका यह कर्तव्य था, कि वह ब्राह्मण अध्यापकों को समुचित धन प्रदान करे, जिससे उनका अध्ययन-अध्यापन का कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहे। निर्धन से निर्धन परिवार का भी यह कर्तव्य था कि वह शिक्षा के निमित्त कुछ न कुछ अंशदान अवश्य करे। उनसे अपेक्षा की जाती थी, कि वे द्वार पर भिक्षा के निमित्त आये ब्रह्मचारी को यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। ब्रह्मचारी को द्वार से वापस करना जघन्य पाप बताया गया है। श्रद्धादि के अवसर पर सामान्यजन विद्वान पंडितों को दक्षिणा प्रदान करते थे।विभिन्न संस्कारों तथा समारोहों के अवसर पर भी उन्हें दान-दक्षिणा दी जाती थी। इस प्रकार समाज का सभी वर्ग शिक्षा को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से यथाशक्ति अंशदान करता था। इससे आचार्यगण आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त होकर पूर्णतया अपने कार्य में तल्लीन रहते थे।
References : 1. पुस्तक- प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, लेखक- के.सी.श्रीवास्तव
India Old Days : Search