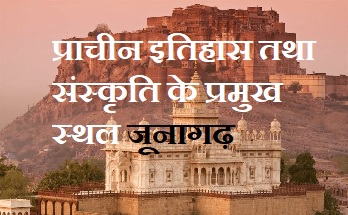राजस्थान में चित्रकला का विकास
राजस्थान में चित्रकला – राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। राजस्थान में चित्रकला के प्रति अभिरुचि और उसका मौलिक स्वरूप परंपरागत रूप से प्रचलित था। कोटा जिले के आलणिया, दरा, बैराठ, आहङ तथा भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों के शैलाश्रयों में आदिम मानव द्वारा उकेरे गये रेखांकन और मृदभांडों की कलात्मक उकेरियाँ इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित करती हैं। परंतु राजस्थानी चित्रकला एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। पूर्व में राजस्थानी चित्रकला को भारतीय चित्रकला एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। पूर्व में राजस्थानी चित्रकला को भारतीय चित्रकला के दायरे में स्वतंत्र अर्थ में ही प्रयुक्त होती है। पूर्व में राजस्थानी चित्रकला को भारतीय चित्रकला के दायरे में स्वतंत्र महत्त्व प्राप्त नहीं था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन 1916 ई. में स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि राजस्थान में भी चित्रकला का एक संपन्न स्वरूप विद्यमान है। डब्ल्यू.एच.ब्राउन ने कुछ चित्रों के नमूनों के आधार पर इसे राजपूत शैली कहा है। लेकिन ए.सी.मेहता ने तो यह मत व्यक्त कर दिया कि ये चित्र हिन्दू शैली के ही हैं। इस प्रकार राजस्थान की चित्रकला को भारतीय चित्रकला के दायरे में स्वतंत्र महत्त्व प्राप्त नहीं हो सका। तदंतर, शनैः शनैः शोधकर्त्ताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह स्पष्ट होता गया कि राजस्थानी चित्रकला को मात्र हिन्दू शैली या राजपूत शैली नहीं कहा जा सकता, वरन् राजस्थानी चित्रकला में अनेक राजपूत शैलियों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब उन शैलियों को मेवाङ, मारवाङ, किशनगढ, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बून्दी, नाथद्वारा आदि शैलियाँ कहते हैं। कुछ विद्वानों ने तो उणियारा शैली और अजमेर शैली को भी उक्त शैलियों से भिन्न माना है। डॉ.गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाङ शैली से भिन्न डूँगरपुर और देवगढ की उप शैलियों का उल्लेख किया है। इन विभिन्न शैलियों के वैज्ञानिक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय चित्रकला के दायरे में राजस्थानी चित्रकला न केवल स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, बल्कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में भी राजस्थानी चित्रकला न केवल स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, बल्कि भारतीय चित्रकला के दायरे में राजस्थानी चित्रकला न केवल स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, बल्कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में भी राजस्थानी चित्रकला का बङा महत्त्व है। राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केन्द्र मेदपाट (मेवाङ) रहा है।

राजस्थानी चित्रकला का विकास
राजस्थान में आहङ, बैराठ, रंगमहल, नोह आदि स्थानों की खुदाई से प्राप्त सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनकाल में राजस्थान में चित्रकला की वैभवशाली परंपरा विद्यमान थी। 7वीं-8वीं शताब्दी के लगभग जब भारत में अजंता चित्रकला परंपरा समृद्ध हो रही थी, तब यहाँ के चित्रकारों ने अजंता चित्रकला शैली में स्थानीय शैलियों को मिलाकर चित्रकला की एक नवीन शैली को प्रारंभ किया। अजंता की चित्रण परंपरा को ग्रहण करने का श्रेय गुहिल वंशीय मेवाङ के शासकों को है। दक्षिणी राजस्थान में मेदपाट (मेवाङ) वह स्थान है जो प्राचीन काल से ही सूर्यवंशी राजाओं के हाथ में रहा है और गुप्त साम्राज्य के विघटन के उपरांत भी भारतीय संस्कृति की मशाल अपने हाथों में लिये रहा। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ (16 वीं शताब्दी) ने मरुप्रदेश (मारवाङ) में 7 वीं शताब्दी में श्रीरंगधर नामक चित्रकार की चर्चा की है। 5 वीं से 12 वीं शताब्दी तक का काल राजस्थान के इतिहास में महत्त्वपूर्ण युग था, अतः यहाँ अन्य कलाओं के साथ चित्रकला भी अवश्य विकसित हुई होगी, किन्तु चित्रों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पाना कठिन है। अजंता चित्रकला शैली में स्थानीय शैलियों को मिलाकर जो नई शैली प्रारंभ की गयी उसके नमूने भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मंडोर द्वार के गोवर्धन धारण और बाङोली तथा नागदा गाँव की मूर्तिकला में इस नई शैली के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। राजस्थान में ताङपत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ सावगपङिकमण सुत्त चुन्नी (श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी) है, जो आहङ (उदयपुर) में सन 1260 ई. में गुहिल तेजसिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। दूसरा प्रमुख उदाहरण मोकल के शासनकाल में देवकुल पाटक (देलवाङा, उदयपुर) सन् 1422-23 ई. में लिखित एवं चित्रित ग्रन्थ सुपासनाह चरित्रम (सुपार्श्वनाथ चरितम्) है। इसमें राजस्थानी चित्रण की भावभूमि पर जैन एवं गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। लगभग 1450 ई. के आसपास पश्चिमी भारत में एक प्रति गीत-गोविन्द और दूसरी बालगोपाल स्तुति की प्राप्त होती है, जिनमें पश्चिमी भारत में एक प्रति गीत-गोविन्द और दूसरी बालगोपाल स्तुति की प्राप्त होती है, जिनमें राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला शैली के अंकुर दिखाई देते हैं। 15 वीं शताब्दी तक, इस प्रकार जो चित्रशैली राजस्थान में प्रचलित रही उस पर जैन शैली, पश्चिमी भारत शैली, अपभ्रंश शैली आदि का पूर्ण प्रभाव रहा। चूँकि अनेक जैन ग्रन्थों के इस शैली में चित्रित किया गया था, अतः इसे जैन शैली कहा गया। आगे चलकर इस शैली के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हो गये। कुछ विद्वानों ने इसे गुजरात शैली, कुछ विद्वानों ने इसे पश्चिम भारतीय शैली और कुछ विद्वानों ने इसे अपभ्रंश शैली की संज्ञा दी। रायकृष्णमदास के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का जन्म हो रहा था, उन दिनों भारत में, गुजरात का सुल्तान महमूद बेगङा तथा मेवाङ के महाराणा कुम्भा दोनों ही कला और कलाकारों को आश्रय दे रहे थे। इसी समय कश्मीर में जैनुल आब्दीन का परम उन्नत व उदार राज्य था। वहाँ चित्रकला उन्नति पर थी, अतः चित्रकला के क्षेत्र में पारस्परिक आदान-प्रदान कोई असंभव बात नहीं थी। राजस्थान में इस नई शैली की अविरल प्रगति होती रही। शैली की दृष्टि से अब राजस्थान और गुजरात में कोई भेद नहीं रह गया था, क्योंकि अनेक गुजराती कलाकार यहाँ आकर बस गये थे, जो सोमपुरा कहलाये। महाराणा कुम्भा के समय सूत्रधार मंडन नामक शिल्पी गुजरात से यहाँ आकर बसा था। इस शैली के चित्रों में कठपुतली की तरह आकृति व चेहरा होता था। संभवतः इस शैली ने राजस्थान की प्राचीन लोककला (कठपुतली) के तत्व ग्रहण कर लिये थे। इस विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में स्थानीय मौलिक परंपरा और अजंता परंपरा के सामंजस्य से उत्पन्न इस नई शैली की अविरल प्रगति होती रही। यद्यपि स्थानीय विशेषताओं के कारण परंपरागत शैली से भिन्न इस नई शैली ने अपना अस्तित्व बना लिया था, तथापि भारतीय चित्रकला के मूल सिद्धांत – षडाङ्ग (छः अंग) का यहाँ निर्वाह होता रहा। चित्रकला के इन छः अंगों का उल्लेख वात्स्यायन ने किया है –
रूपभेद प्रमाणानि भावलावण्य योजनाम्
सादृश्य वर्णिकाभंग इति चित्र षङ्गाङ्गकम्।।
अर्थात् प्रत्येक चित्र में रूपभेद (बनावट का स्वरूप), प्रमाणानि (आकार वगैरह), भावलावण्य (भावपूर्ण सौन्दर्य), योजनानि (चित्र की आजोजना वगैरह), सादृष्य (अनुरूपता) और वर्णिकाभंग (रंगों का संयोजन) इन छः अंगों का निर्वाह होता रहा। यहाँ तक कि 19 वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला में भी इनका निर्वाह दिखाई देता है। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 16 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के बीच 1500 ई. के लगभग माना जाना चाहिये। गुजरात और मेवाङ में जिस समृद्धशाली शैली के उदयस्वरूप भारतीय चित्रकला की प्रसुप्त चेतना उद्भूत हुई थी वह अपभ्रंश शैली का ही नवीन संस्करण थी। भाव-विधान एवं आलेखन की दृष्टि से राजस्थानी शैली यद्यपि अपने अपूर्व नये परिवेश को लेकर आई थी, किन्तु विषय वस्तु के लिये उसने अपनी पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली का ही आश्रय लिया। इस शैली के चित्रों में कठपुतली की तरह चेहरा, तीखी नाक, नुकीली दोहरी ठुड्डी तथा अनुपात में बङी आँखें होती थी। इन चित्रों में मुख्य रूप से लाल रंग व नीले रंग को मिलाकर एकरंगी पृष्ठभूमि बनाई जाती थी तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिकता से होता था।
15 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लोदी सुल्तानों के समय राजस्थानी चित्रकला के विकास में एक नया मोङ आया। यद्यपि गुजरात या जैन शैली का प्रभाव तो यथावत रहा, लेकिन अब अनुपात से बङी आँखों का चित्रण, जो जैन शैली की एक विशेषता थी, समाप्त होने लगा।तत्कालीन वेशभूषा दर्शायी जाने लगी, दैनिक जीवन के चित्र बनने लगे तथा भिन्न-भिन्न रंगों का प्रयोग कर चित्र को रंग-विरंगा बनाया जाने लगा। अब प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन भी होने लगा। अब तक केवल जैन व हिन्दू धर्म-ग्रन्थों को ही चित्रित किया जाता था, लेकिन अब फारसी ग्रन्थों को भी स्थानीय चित्रकारों द्वारा चित्रित कराया जाने लगा। इन ग्रन्थों की चित्रकला में फारसी व भारतीय शैली का मिश्रण पाया जाता है। अब गैर-धार्मिक ग्रन्थों को भी चित्रित करने का प्रचलन आरंभ हो गया। इस काल के चित्रों में यद्यपि गुजरात या जैन शैली की प्रधानता रही, किन्तु कुछ नवीन तत्वों का समावेश भी हुआ। पुरुष आकृति को कून्हा पगङी (फैली हुई) पहने हुए दिखाया जाने लगा। अतः इस श्रेणी के चित्रों को कून्हेदार समूह के चित्र कहा गया। कुछ विद्वान इन चित्रों को मेवाङी चित्रों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि मेवाङ के लघु चित्रों में पगङी का प्रयोग लोदी सुल्तान और उनके अधीन हिन्दू शासक ही करते थे और ऐसी पगङी का राजस्थान में कभी प्रचलन नहीं रहा। अतः खंडालवाला ने इस चित्रकला को लोदी शैली कहा है। लोदी चित्रकला दरबारी कला नहीं थी बल्कि इस कला के संरक्षक हिन्दू, मुसलमान, साहित्य में रुचि रखने वाले संभ्रान्त लोग और धार्मिक विचारों वाले व्यापारी थे। 1526 ई. में यद्यपि लोदी सुल्तानों का पतन हो गया था, फिर भी 1562 ई. तक कुछ न कुछ अंशों तक यह लोदी शैली प्रचलित रही।
मुगल शैली का प्रभाव
16 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजस्थान की चित्रकला शैली में पुनः महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। 1567 ई. में मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबारी चित्रकारों – मीर सैय्यद अली व अब्दुस्समद को हमजानामा चित्रित करने का काम सौंपा। इस प्रयोजना में 1,400 बङे प्रतिभाशाली चित्रकारों को बुलाया गया। 1582 ई. तक प्रयोजना का कार्य चलता रहा। कार्य समाप्त होने पर राज्यों से आये चित्रकार पुनः अपने राज्यों में चले गये। लेकिन लंबे समय तक ईरानी चित्रकारों के निर्देशन में कार्य करने से उन्होंने चित्रकला के नये तत्व ग्रहण कर लिये थे, जिनका प्रयोग उन्होंने अपने राज्य में बनाये गये चित्रों में किया। यद्यपि आरंभ में उन चित्रों पर गुजरात शैली व लोदी शैली का प्रभाव व मुगल वेश भूषा की प्रधानता रही, लेकिन ज्यों-ज्यों राजपूत शासकों ने मुगल सम्राट से राजनैतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित कर, मुगल दरबार में निरंतर आना जाना किया, राजस्थानी चित्रकला में मुगल प्रभाव अधिकाधिक बढता गया। फलस्वरूप राजस्थान की मूल शैली समाप्त होने लगी तथा चित्रकला की मुगल तकनीक के प्रति रुचि बढने लगी। इसलिए प्रो. हीरेन मुखर्जी की मान्यता है कि राजपूत शैली का जन्म मुगल चित्रकला शैली से हुआ था। किन्तु यह मात्र भ्रांति है, क्योंकि इस काल में मुगल प्रभाव होते हुए भी राजपूत शासकों की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अतः राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला से स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकी। कार्ल खंडालवाला ने बीकानेर में उपलब्ध इस काल के कुछ चित्रों का उल्लेख करते हुए बताया है कि यद्यपि ये चित्र मुगल शैली के अधिक निकट प्रतीत होते हैं, फिर भी ये चित्र स्थानीय विशेषताओं के कारण मुगल शैली से भिन्नता बताते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी प्रकट करते हैं।
समय के साथ-साथ राजस्थानी नरेशों एवं मुगल सम्राट के बीच समागम बढता गया, जिससे राजस्थानी चित्रकला मुगल प्रभाव में विकसित होने लगी। मेवाङ के महाराणा अमरसिंह ने 1605 ई. में चावंड में रागमाला चित्रित करने के लिये नासिरुद्दीन नामक एक मुस्लिम चित्रकार को आमंत्रित किया था। इस समय के बने रागिनी और भागवत के चित्र चमकदार रंगों, चेहरों की कोणीयता और वेश-भूषा की दृष्टि से गुजरात शैली के लगते हैं, लेकिन लोदी और मुगल शैलियों का आंशिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस नयी शैली में स्थानीय विशेषताएँ सम्मिलित होने के कारण 17 वीं और 18 वीं शताब्दी में राजस्थान में मेवाङ, मारवाङ, बूँदी, कोटा, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, आमेर और बाद में जयपुर आदि राज्यों में नयी शैलियाँ विकसित होने लगी। कार्ल खंडालवाला ने 17 वीं शताब्दी और 18 वीं शथाब्दी के आरंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा है। इसके बाद यद्यपि कुछ उत्कृष्ट चित्र तो बने हैं, किन्तु चित्रकला अपने पराभव की ओर अग्रसर होती दिखाई देती है।
चित्रकला के इस पराभव के युग में भी हमें कुछ अपवाद दिखाई देते हैं। किशनगढ का महाराजा सावंतसिंह (1699-1764 ई.) जो हिन्दी काव्य साहित्य में नागरीदास के नाम से विख्यात है, न केवल उच्चकोटि का कवि और कला का संरक्षक ही था, बल्कि वह स्वयं एक दक्ष चित्रकार भी था। महाराजा सावंतसिंह के निर्देशन में निहालचंद नामक चित्रकार ने 1737 से 1760 ई. तक कार्य किया। सावंतसिंह और निहालचंद द्वारा निर्मित उच्चकोटि के चित्रों से एक स्वतंत्र चित्रकला की शैली का निर्माण हुआ, जिसने कला जगत में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। मेवाङ में 1628-1653 ई. तक साहेबदीन नामक मुस्लिम चित्रकार एवं उसकी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। साहेबदीन मुगल दरबार में दरबारी चित्रकारों के निर्देशन में कार्य कर चुका था, अतः उसके द्वारा निर्मित चित्रों में मुगल दरबार में दरबारी चित्रकारों के निर्देशन में कार्य कर चुका था, अतः उसके द्वारा निर्मित चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन चित्रों की बनावट और रंगों के प्रयोग में उसका स्वयं का व्यक्तित्व दिखाई देता है। अतः उसने मेवाङी चित्रकला को एक नयी दिशा दी। साहेबदीन द्वारा प्रतिपादित शैली भागवत, पुराण, रामायण, रागमाला, गीत गोविन्द आदि ग्रन्थों के चित्रण में भी मिलती है। 1740 ई. के आस-पास चित्रित महाभारत के 3,000 चित्रों में भी यही शैली दिखाई देती है, लेकिन साहेबदीन के समय के विशिष्ट लक्षण और आभा दिखाई नहीं देती।
मेवाङी चित्रकला शैली ने राजस्थान के लगभग सभी चित्रकला केन्द्रों को न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित किया था और इस प्रभाव के अंतर्गत प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वयं की शैली भी विकसित की। बूँदी के चित्रों में हम पेङ-पत्तियों के गुच्छे, बहते हुए पानी, पानी के जीव-जन्तु, स्थापत्य का प्रदर्शन करते हुये टाइल्स की दीवारें और फर्श आदि की प्रधानता देखते हैं। स्रियों की आकृतियों में उनका चेहरा छोटा और गोलाकृति में मस्तिष्क अपनी विशेषताएँ लिये हुए हैं। 1760 ई. के बाद बँदी के चित्रों में मुगल प्रभाव अधिक दिखायी देता है, जिसमें चेहरे पर अत्यधिक गहरा रंग और ऐसे विषय जिन पर मुगल शैली में चित्र बनते थे, जैसे – लैला-मजनू का प्रणय चित्र आदि। विषयों और आकृतियों की दृष्टि से बूँदी और कोटा के चित्रों में भेद करना अत्यन्त कठिन है, लेकिन 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से कोटा के चित्रों में शिकार के दृश्यों की प्रधानता दिखायी देती है। बूँदी और कोटा दोनों की चित्रकला में हाथियों की लङाई के चित्र आमतौर पर प्रचलित थे। बीकानेर में बने चित्रों में मुगल शैली की प्रधानता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीकानेर के मुख्य चित्रकार अधिकांश काल तक मुसलमान ही रहे, लेकिन बीकानेर के चित्र भी अपनी स्वयं की विशेषता लिये हुए हैं। सिरोही की चित्रकला में मेवाङी शैली का प्रभाव अधिक दिखायी देता है। लेकिन रंग योजना मेवाङी शैली की अपेक्षा समृद्ध दिखायी देती है। मारवाङ में प्रारंभिक चित्रकला अधिक प्रभावशाली दिखायी देती है, जैसे – जोधपुर दुर्ग में चोकेलाव महल में मालदेव के काल में बने राम रावण युद्ध के दृश्य अत्यधिक प्रभावशाली हैं। 1624 ई. के आस-पास पाली में चित्रित रागमाला भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके बाद तो मारवाङ की चित्रकला और भी अधिक समृद्ध हुई है। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वयं की शैली विकसित की, उसकी अपनी अलग पहचान है और स्वयं ही अलग से रंग योजना है, जिससे वे सभी अपना-अपना अस्तित्व प्रकट करती हैं।
18 वीं शताब्दी मुगलों की शक्ति के पराभव का युग था। परंतु यह युग ऐश्वर्य और विलास-वासना का था। शक्तिहीन मुगल सम्राट के दरबार से मुँह मोङकर राजस्थानी नरेश अपनी राजधानियों में वापस लौट आये। संरक्षण के अभाव में वहाँ के कलाकार भी राजस्थानी राज्यों में आ बसे। राजस्थानी नरेशों का प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने राजस्थानी शैली को सर्वथा नूतन स्वरूप प्रदान किया। चूँकि यह युग राजस्थान में असीम ऐश्वर्य और विलास वासना का था, अतः इसका प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर भी पङना स्वाभाविक था। इस प्रभाव के फलस्वरूप अब शासकों के ऐश्वर्यपूर्ण एवं विलासी जीवन के दृश्यों पर जोर दिया जाने लगा, जैसे – शासक को अपने दरबारियों के साथ दिखाना, शासक के शिकार के दृश्य, दरबार में संगीत तथा नृत्य का आयोजन आदि। निः संदेह इस प्रकार के चित्रों की विचारधारा मुगलों से ग्रहण की गयी थी। 18 वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी चित्रकला में मुगल शैली पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। अतः इस काल के चित्रों में मुगल शैली को ढूँढना प्रायः असंभव हो गया, जिससे इस काल के चित्रों में राजस्थानी शैली का विशुद्ध रूप दिखायी देने लगा। उस युग में कृष्ण-लीला और राधा-कृष्ण संबंधी धार्मिक चित्रों में भी मानवीय कामुकता का ही चित्रण होता था। चित्रकला की यह प्रवृत्ति केवल राजस्थानी शासकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सामंत भी अपनी जागीर की हवेली में चित्रकारों का प्रश्रय देने लगा। ऐसे सामंतों में घाणेराव, देवगढ, उणियारा, शाहपुरा, बदनौर, सलूम्बर, कोठारिया आदि के सामंत प्रमुख हैं। इसमें से कुछ ठिकानों की चित्रकला पर शोध कार्य हो रहा है।
19 वीं शताब्दी के प्रारंभ से राजस्थानी शैली पर बने चित्रों में भाव-चित्रण की निर्जीवता आने लगी। इस काल में राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश अंकुश बढता गया। अँग्रेजों को भारी खिराज चुकाने के फलस्वरूप शासकों की आर्थिक स्थिति बिगङती जा रही थी तथा राजस्थान की सदियों पुरानी संस्कृति को गहरी ठेस पहुँच रही थी। शासकों की इस बिगङती हुई स्थिति के कारण राजस्था के चित्रकारों को इस काल में पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। फलस्वरूप चित्रकारों ने अपनी आजीविका हेतु व्यावसायिक चित्रकला को अपना लिया। चित्र शैली की प्रचलित रूढियों के विपरीत नित्य नये वैषम्यपूर्ण प्रयोग किये जाने लगे, जिससे यहाँ की कला का परंपरागत विकास सर्वथा अवरुद्ध हो गया। फिर भी यत्र-तत्र रजवाङे अपनी शैलियों को जीवित रखने में समर्थ हो सके, लेकिन चित्रकला जगत में इसे अपवाद ही कहा जायेगा। व्यावसायिक चित्रकला में मात्र छिछलापन ही दिखायी देता था।
राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ
- मेवाङी चित्रकला की शैली
- मारवाङ चित्रकला शैली
- बीकानेर चित्रकला शैली
- किशनगढ चित्रकला शैली
- जयपुर चित्रकला शैली
- बूँदी चित्रकला शैली
- कोटा चित्रकला शैली
अन्य शैलियाँ
इन सभी मुख्य शैलियों के अलावा राजस्थान में अलवर शैली, उणियारा शैली और नाथद्वारा शैली का भी अपना महत्त्व है। अलवर शैली में मुगल प्रभाव की अधिक प्रधानता दिखाई देती है। यद्यपि उणियारा, जयपुर राज्य की एक जागीर थी, लेकिन उणियारा के चित्रों में आँखों की बनावट, जयपुर शैली से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार नाथद्वारा मेवाङ राज्य से संबंधित होते हुए भी नाथद्वारा के चित्र, मेवाङी शैली से भिन्न अपनी विलक्षणता लिये हुए हैं। सन् 1671 ई. में जब ब्रज से श्रीनाथजी की मूर्ति यहाँ लायी गयी उस समय ब्रज में बसने वाले अनेक चित्रकार भी यहाँ आकर बस गये और श्रीनाथजी की छवि बनाने लगे। धीरे-धीरे नाथद्वारा वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केन्द्र बन गया, फलस्वरूप श्रीनाथजी की छवि के चित्रों की माँग बढने लगी जिसने अन्य राज्यों के चित्रकारों को भी यहाँ आकर बसने के लिए प्रेरित किया। चित्रों के विषय वही अर्थात् श्रीनाथजी की छवि, गुसाइयों के दैनिक जीवन तथा उनको श्रीनाथजी की पूजा करते हुए दिखाना और कृष्ण-लीला ही रहे, लेकिन इसमें राजस्थान के तथा अन्य उत्तरी भागों की शैलियों का समावेश हो गया। फलस्वरूप एक नयी नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव हुआ। 18 वीं शताब्दी में बने चित्रों में श्रीनाथजी, यमुना – स्नान, हिंडौला (कृष्ण के बाल स्वरूप को झूले में दिखाना), जन्माष्टमी, अन्नकूट आदि उत्सवों के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इन चित्रों में गहरे नीले, पीले और सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। 19 वीं शताब्दी में नाथद्वारा शैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर उन्मुख हो गयी, जिससे उन चित्रों में मौलिकता होते हुए भी वह रोचकता नहीं रही जो हमें 18 वीं शताब्दी के चित्रों में दिखाई देती है।
सभी शैलियों पर एक दृष्टि
राजस्थान की इन सभी शैलियों के अध्ययन से एक बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि इन शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी उनमें मौलिक एकता है। प्रारंभ के सभी शैलियों के चित्रों में अजंता परंपरा शैली के दर्शन किये जा सकते हैं। विषयों के चयन में राग-रागिनी, बारहमासा, भागवत पुराण, रामायण, गीत गोविन्द, राधा-कृष्ण, रासलीला आदि भी सभी शैलियों में दिखाये गये हैं। स्रियों की वेश भूषा स्थानीय परंपरा के अनुकूल होते हुए भी उनके आभूषणों में साम्यता देखी जा सकती है। श्रृंगारी चित्र भी सभी राज्यों के प्रमुख विषय रहे हैं। सभी शैलियों में मुगल शैली का प्रभाव, मुगलों की शानशौकत और विलासिता देखी जा सकती है। 19 वीं शताब्दी के अंत में सभी शैलियाँ यूरोपीय कला से प्रभावित होकर व्यावसायिक कला के रूप में परिवर्तित हुई थी। सभी राज्यों की चित्रकला में हम तत्कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
References : 1. पुस्तक - राजस्थान का इतिहास, लेखक- शर्मा व्यास